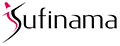हिन्दी साहित्य में लोकतत्व की परंपरा और कबीर- डा. सत्येन्द्र

हिन्दी साहित्य में लोकतत्व की परंपरा और कबीर- डा. सत्येन्द्र
भारतीय साहित्य पत्रिका
MORE BYभारतीय साहित्य पत्रिका
हिन्दी पहले लोक भाषा थी। लोकभाषा ही शनैः शनैः साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण करती है। लोक-भाषा में जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं उनमें सहज ही लोकतत्व रहता है। फलतः हिन्दी के आरंभकालीन काव्य में लोक-तत्व मिलना ही चाहिये, हमें इसी लोक-तत्व का अनुसंधान करना है।
किन्तु यह बात स्पष्ट विदित होती है कि हिन्दी में लोक-भाषा से साहित्य की ओर कदम बढ़ाया, पर लोक-भाषा के अपने स्वाभाविक स्वरूप को बहुत काल तक अक्षुण्ण रखा। साहित्य-रचना में प्रवृत्त होने पर भी उसने लोक-संपर्क घनिष्ठ बनाये रखा। लोक-संपर्क की घनिष्ठता के कई कारण विदित होते हैं।
एक कारण यह है कि हिन्दी ने जब से जन्म ग्रहण किया तभी से भारत में बहुत अधिक उथल-पुथल रही। इतिहास भी बदलता रहा, इतिहास की नीति बदलती रही। साँस्कृतिक संघर्ष हुए, आन्दोलन चलते रहे- ये समस्त विकृतियाँ चंचल उत्तुंग तरंगों की भाँति उत्पन्न हुई, इन्होंने साहित्य में अपनी सत्ता प्रकट की, और साहित्य की इन्हीं तरंगों के कारण लोक-संपर्क को आधार के रूप में बार-बार ग्रहण करना पड़ा। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उद्वेलन जब तक चलते रहे, साहित्य का लोक-संपर्क घनिष्ठ बना रहा और जब ये उद्वेलन शिथिल हो गये तभी साहित्य ने युग-युगीन प्रवृत्ति को प्रकट करने वाले साहित्य के रूप को स्थिरता-पूर्वक अपना लिया।
सातवीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक ये उद्वेलन चले। हर्ष की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास का प्राचीनकाल समाप्त हुआ, और मध्यकाल अवतीर्ण हुआ। मध्यकाल के अवतीर्ण होने के कई अर्थ हैं- इस नये अवतारणा से नये जीवन-मान प्रस्तुत होने ही चाहिये। नये अभिव्यक्ति के माध्यम प्रबल होंगे और, अभिव्यक्तियों की कला का स्वरूप और सामग्री भी परिवर्तित होगी। ये परिवर्तन और अभिव्यक्तियाँ क्या थीं। संक्षेप में यहाँ उनका उल्लेख करना उचित हैः-
1. इस बीच धीरे-धीरे तत्सम-बहुल रूप प्रकट होने लगा था। नवीं-दसवीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों के प्रवेश का प्रमाण मिलने लगता है और चौदहवीं शताब्दी से तो तत्सम शब्द निश्चित रूप से अधिक मात्रा में व्यवहृत होने लगे। क्रियाएं और विभक्तियाँ तो ईषत् विकसित या परिवर्द्धित रूप में बनी रही पर तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़ जाने से भाषा भी बदली-सी जान पड़ने लगी। (हि. सा. का आ. का. पृष्ठ 17)
इसका अभिप्राय है कि तद्भव-प्रधान की प्रवृत्ति को हटाकर भाषा ने तत्सम प्रधानता का मार्ग ग्रहण किया, और इस काल में यह प्रवृत्ति उत्तोरत्तर बढ़ती गयी, जिससे भाषा ही बदल गयी। भाषा में यह प्रवृत्ति क्यों आयी?
डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी के मत से दो कारण हैं -
अ. भक्ति के नवीन आन्दोलन के कारण। इससे भागवत पुराण का प्रभाव विशेष पड़ा।
आ. शांकरमत की दृढ़ प्रतिष्ठा के कारण।
2- ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर काव्य लिखने की प्रथा बाद में खूब चली। इन्हीं दिनों ईरान के साहित्य में भी इस प्रथा का प्रवेश हुआ। उत्तर-पश्चिम सीमान्त से बहुत-सीं जातियों का प्रवेश होता रहा- पता नहीं उन जातियों तो स्वदेशी प्रथा की क्या क्या बातें इस देश में चलीं। साहित्य में नये-नये काव्य रूपों का प्रवेश इस काल में हुआ अवश्य। सम्भवतः ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर काव्य लिखने या लिखाने का चलन भी उनके संसर्ग का फल हो। परन्तु भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया, शैली उनकी वही पुरानी रही जिसमें काव्य-निर्माण की ओर अधिक ध्यान था--(वही-पृ. 70)
अभिप्राय यह है कि इस युग में नये काव्यरूपों की उद्भावना हुई जिसमें से एक रूप वह था जिसमें ऐतिहासिक आश्रय और नाग लेकर काव्य-कल्पना का कौतुक प्रकट किया जाता था।
3—संदेश रासक में कवि ने जिस बाह्य प्रकृति के व्यापारों का वर्णन किया है वह रासो के समान ही कविप्रथा के अनुसार है। उन दिनों ऋतु-वर्णन के प्रसंग में वर्ण्य वस्तुओं की सूची बन गई थी। बारहवीं शताब्दी की पुस्तक कवि कल्पलता में और चौदहवीं शताब्दी की पुस्तक वर्णरत्नाकर में ये नुस्खे पाए जा सकते हैं। इन बाह्य वस्तु और व्यापारों के आगे न तो रासो का कवि गया है, न अद्दहमान ही। (वही-पृ. 84)
इससे विदित होता है कि काव्य-रचना में विशेषतः बाह्य अथवा प्राकृतिक वर्णनों में कवि-प्रथा का अनुसरण होता था। कवि नयी उद्भावनाएँ नहीं कर सकता था।
4—नया छन्द नये मनोभाव की सूचना देता है। श्लोक लौकिक संस्कृत के आविर्भाव का सन्देशवाहक है। जिस प्रकार श्लोक संस्कृत की मोड़ का सूचक है उसी प्रकार गाथा, प्राकृत की ओर के झुकाव का व्यंजक है।.....तीसरे झुकाव की सूचना लेकर एक दूसरा छंद भारतीय साहित्य के प्रांगण में प्रवेश करता है। यह दोहा है। स्पष्ट ही दोहावंश का अर्थ अपभ्रंश है। अपभ्रंश को दूहाविद्या कहा गया है। (वही पृ. 90-92)
दोहा नये युग की उद्भावना से संबंधित है।
5- दोहा, वह पहला छंद है, जिसमें तुक मिलाने का प्रयत्न हुआ और आगे चल कर एक भी ऐसी अपभ्रंश-कविता नहीं लिखी गई जिस में तुक मिलाने की प्रथा न हो। इस प्रकार अपभ्रंश केवल नवीन छंद लेकर ही नहीं आई, बिल्कुल नवीन साहित्यिक कारीगरी लेकर भी आविर्भूत हुई। (वही पृ. 93)
6- दोहे को प्रबंध-काव्य के योग्य बनाने के लिए चौपाई का उपयोग किया गया। इसी कथानक सूत्र को जोड़ने के उद्देश्य से सोलहवीं शताब्दी में दोहों के बीच-बीच में चौपाई जोड़कर कथानक का क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया था। (वही पृ. 94)
7. इस काल में उद्भावित काव्य रूप-
1. आदि मंगल (मंगल काव्य)
2. रमैनी (चौपाई दोहे)
3. शब्द (गेय पद)
4. ग्यान चौंतीसा (वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से आरंभ करके पद लिखना)
5. विप्रगतीसी
6. कहरा
7. बसन्त
8. चाँचर
9. बेलि
10. बिरहुली (सांप का विष उतारने वाला गान)
11. हिंडोला
12. साखी (दोहे)
13. दोहा-चौपाई वाला चरित काव्य
14. कवित्त-सवैया
15. दोहों में अध्यात्म और धर्म-नीति के उद्देश्य
16. बरवै
17. सोहर छन्द
18. विनय के पद
19. लीला के पद
20. वीर काव्यों के लिए उपयोगी छप्पय, तोमर, नाराच आदि की पद्धति
21. दोहों में सगुन विचार
22. फागु
23. अखरावट (वही. पृ. 104, 101, 107)
24. नहछू
25. रासक
26. रास
27. रासो
28 कुंडलिया
29. भ्रमरगीत
30. मुकरी
31. दो सखुने
32. बुझौवल
33. षटऋतु
34. बारह मासा
35. नखशिख
36. दशावतार
37. भंड़ौआ
38. जीवनी काव्य
यह मध्ययुग के साहित्य रूपों और उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। इस से यह स्पष्ठ हो जाता है कि मध्ययुग साहित्य के लिए कितने ही परिवर्तनों को लेकर अवतीर्ण हुआ। इन परिवर्तनों के मूल में कितने ही उद्वेलन थे जिन्हें यहाँ गिनाया जाता है---
1. भक्ति आन्दोलन
2. नाथ-संप्रदाय
3. संत-संप्रदाय
4. सिद्ध-संप्रदाय
5. शाक्त-मत
6. वैष्णव-संप्रदाय
7. सूफी मत
8. राम संप्रदाय
9. कृष्ण-संप्रदाय
10. राधा संप्रदाय
11. जैन-मत
12. सहजयान
13. वज्रयान
14. इस्लाम आदि
हमें जिस युग का अध्ययन करना है वह भक्ति आन्दोलन की दूसरे तथा तीरसे चरण से संबंधित है। भक्ति आंदोलन के पाँच चरण प्रतीत होते हैं—
1. संधि-चरण- भक्ति का हिंदी क्षेत्र में आरंभ। बीजारोपण
2. अंकुरण- अंकुर जिस प्रकार भूमि से संबद्ध रहता हुआ भी उससे ऊपर अपने व्यक्तिगत स्वरूप के अभिमान से लहलहाने लगता है, उसी प्रकार भक्ति अपने थाले में से बाहर फूटी- निर्गुणोपासक संत संप्रदाय की भक्ति का यही रूप मानना होगा।
3. प्रेमाभिसारण
4. अवताराश्रयी-चरमोत्कर्ष
5. स्थिरत्व।
भक्ति के विकास की इस द्वितीय स्थिति तक पहुँचते पहुँचते युग की प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन प्रस्तुत हुए, उनका मूल तत्व था वैविध्यका साधारणीकृत एकत्व और उसकी वैष्णवत्व में समर्पित होने की चेष्टा। यह स्थिति विकास और विवर्तन का परिणाण थी। भारत में मत-स्वातंत्र्य की सुविधा होने के कारण प्रत्येक युग में यहाँ अनेकों मत तथा संप्रदाय रहे हैं, और वे साथ-साथ चलतेरहे हैं। पहले वैदिक धर्म ने प्रबलता प्राप्त की।
विशेष रोचक बात यह है कि ये सभी संप्रदायवादी एक ही आश्रय में एक साथ रहते थे। (हर्ष रचितः डा. वासुदेवशरण अग्रवाल)
फिर बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म के उपरान्त धार्मिक क्षेत्र में हमें जो प्रवृत्ति मिलती है, वह वस्तुतः एक नयी प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति सु-संबद्ध समन्वित महत्व की प्रवृत्ति कही जा सकती है। वैदिक धर्म ने शिश्न देवों को घृणा की दृष्टि से देखा। बौद्धौं ने अपने से इतर समस्त मतानुयायियों को हीन समझा। किन्तु जो नया युग प्रवर्तित हुआ वह उस धर्म को लेकर उठा जिसे आज हिन्दू धर्मि कहते है। पहली अवस्था में वे समस्त मत समन्वित होते प्रतीते होंगे जो बौद्ध-धर्म से विरोध रखते थे, दूसरीं अवस्था में इस उदार भावना ने स्वयं बुद्ध को आत्मसात कर लिया और बौद्ध धर्म भी समन्वित हो गया। इस समन्वय को लाने के लिए एक ऐसी दार्शनिक भऊमिका प्रस्तुत करनी पड़ी जिसने एक दूसरे से भिन्न संप्रदायों की मान्यताओं को परस्पर सुसंबद्ध करने का प्रयत्न किया। यह लोक-प्रवृत्ति का परिणाम था।
इस नयी क्रान्ति से हमें अपने आलोच्य युग तक पहुँचते पहुँचते तीन चरण मिलते हैः—
प्रथम-वैष्णव
द्वितीय- शैव
तृतीय- सिद्ध
चतुर्थ-नाथ
पंचम-भक्ति
प्रथम वैष्णव चरण ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दू धर्म के नाम से भी अभिहित किया जा सकता है, और इसका ऐतिहासिक उत्कर्ष ईसवीं की पहली दूसरी शताब्दी तक माना जा सकता। इस उत्कर्ष में वैष्णव धर्म ने समस्त बौद्ध विरोधी संप्रदायों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयत्न किया। यह सहज ही समझा जा सकता है कि यह प्रयत्न वेदों को ही आगे करके बढा होगा। क्योंकि बौद्ध धर्म जिस प्रबल संप्रदाय के विरुद्ध खड़ा हुआ था, वह मुख्यतः वैदिक था। बौद्ध धर्म दुर्बल हुआ तो वेदों की प्रतिष्ठा को फिर बढ़ाने का प्रयत्न हुआ, किन्तु इतनी शताब्दियों का व्यवधान विवश कर रहा था कि वेदों के समस्त योग-दान को नयी प्रकार से प्रस्तुत किया जाय। पुराणसाहित्य में हमें वह प्रयत्न दिखाई पड़ता है। अतः प्रथम वैष्णव चरण का मूलाधार वैदिक व्याख्या थी।
दूसरा चरण पूर्ण उत्कर्ष पर दशवीं शताब्दी में पहुँचा। इसका दृष्टिकोण वैष्णव दृष्टिकोण से भिन्न था। यह अवैदिक था। डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है—
“कहने का तात्पर्य यह है कि गोरक्षनाथ के पूर्व ऐसे बहुत से शैव, बौद्ध और शाक्त संप्रदाय थे जो वेद बाह्य होने के कारण न हिन्दू थे और न मुसलमान। जब मुसलमानी धर्म प्रथमवार इस देश में परिचित हुआ तो नाना कारणों से देश दो प्रतिद्वन्द्वी, धर्मसाधना-मूलक दलों में विभक्त हो गया। जो शैव मार्ग और शाक्त मार्ग वेदानुयायी थे, वे वृहत्तर ब्राह्मण प्रधान हिन्दु समाज में मिल गये और निरंतर अपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे।“ (वही-पृ. 147) शेष वेद-बाह्य संप्रदाय गोरख संप्रदाय में अन्तर्भुक्त हुए, किन्तु वे ही जो योग को मानते थे। “जो लोग वेद विमुखता और ब्राह्मण विरोधिता के कारण समाज में अगृहीत रह जाते, वे उन (गोरखनाथ) की कृपा से ही प्रतिष्ठा पा सकते थे। (वही पृ. 163)
इस प्रकार नाथ संप्रदाय ने बिखरे संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोने का कार्य संपादित किया। नाथ संप्रदाय दसवीं शताब्दी में चरमोत्कर्ष पर पहुँच कर ह्रास की ओर अग्रसर हुआ।
तभी भक्ति आंदोलन उठा। यह वैष्णव आन्दोलन का ही नया संस्करण था। इसने समस्त लौकिक-वैदिक तत्वों को समन्वित करने का प्रयत्न किया। भक्ति की भावना, अवतार में आस्था, निर्गुण-सगुण का समन्वय, सहज-सुरति औऱ योग की योजना, पूजा कीर्तन और काव्य का उपयोग, नाम और रूप का आश्रय- ये सभी प्रमुखतः लोक तत्व हैं, जिनके पोषण के लिए वेद-उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का आधार ग्रहण किया गया। वस्तुतः वेदों का आश्रय तो प्रमाणार्थ ही लिया गया, इस भक्ति आन्दोलन का समस्त रूप और आत्मा लोक-तत्वों से निर्मित थी। इस नये आन्दोलन ने वैदिक-अवैदिक समस्त भारतीय सांप्रदायिक प्रवृत्तियों का एकीकरण कर दिया, इनमे वैष्णवीय अहिंसा अथवा दाक्षिण्य की भावना प्रधान हो गयी, अतः केवल उग्र शाक्त ही इसमें नही समा सके। ये उग्रशाक्त लोक ग्राह्य नहीं थे। भक्ति की इस नयी अवतारणा के दाक्षिण्य ने मुसलमानों को भी अग्राह्य नहीं माना।
हरि को भजै सो हरि कौ होई।
यह मनोवृत्ति प्रधान हो चुकी थी।
हिन्दी में इसका प्रबल उद्घोष कबीर न किया। कबीर में लोक-भूमि अत्यन्त स्पष्ट और अत्यन्त प्रबल है, कबीर को हिन्दी में संतमत का प्रवर्तक माना जाता है। हमें संतमत के साहित्य में लोक-तत्वों की प्रधानता मिलती है। अब यह आवश्यक है कि कबीर के संदंध में जो प्रमुख दृष्टियाँ रही हैं, उन्हें समझ लिया जाय-
विद्वान चंद्रबली पांडे जी ने सिद्ध किया है कि कबीर जिन्दीक अर्थात सूफी थे। वे जन्म से मुसलमान ही नहीं थे, सूफी मत से मुसलमानी विश्वासों को मानने वाले थे, और उन्हें उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया हैः-----
कबीर चाल्या जाइ था, आगैं मिल्या खुदाइ,
मीराँ मुझ सौं यौं कह्या, किनि फुरमाई गाइ?
गाफिल गरब करें अधिकाई, स्वारथ अरथि बधैं ये गाई।
जाकौ दूध धाइ करि पीजे, ता माता का वध क्यूं कीजै
लहुरैं थकें दुहि पीया खीरो, ताका अहमक भखै सरीरो।
इनमें गौबध करने का निषेध कुरान के उस मत से संबंधित है, जिसमें गोबध को वैध नहीं बताया गया।
एक अचंभा देखिया बिटिया जायौं बाप।
बाबल मेरा ब्याह करि, वर उत्यम ले चाहि।
जब लग वर पावैं नहीं, तब लग तँही ब्याहि।
ये सूफी संस्कार हैं (देखियेः स्टडीज इन् इसलामिक मिस्टीसीज्म, पृ. 113)
कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाउँ।
गले राम की जेवड़ी, जित खैचैं तित जाउँ।।
यह कुत्ते की उपमा कल्बे मुस्तफा और कल्बे अब्बास का फल है।
कलि का स्वामी लोभिया, मनसा धरी बधाइ।
दैहिं पईसा ब्याज कौं, लेखां करता जाइ।।
इसमें सूद न लेने की इसलामी शिक्षा है।
सात समंद की मसि करौं लेखनि सब बन राइ।
धरती सब कागद करौं, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ।।
यह कुरान की आयत का तर्जुमा है। (देखिये सू. लुकमान , डा. नजीर का अनुवाद)
हमरे राम रहीम करीमा केसो, अलह राम सति सोई।
यह भाव भी कुरान से है-(दे. सू. बनी इस्माईल 17, पा. सुब्हानल्लज़ी 15
या करीम बलि हिकमति तेरी खाक एक सूरति बहुतेरी
अर्ध गगन में नीर जमाया, बहुत भांति करि नूरनि पाया।
अवलि आदम पीर मुलांना, तेरी सिफति करि भए दिवाना।
कहै कबीर यहु हेत विचारा, या रब या रब यार हमारा।
(देखिये सू. नूर 24, पा. क़द अफ़्लहल मोमिनून, पृ. 499 तथा सू. फातिर 35, पा. वमैं यक्नुत 22, वही पृ. 108)
पांडे न करसि वाद विवादं, या देही बिन सबद न स्वादं
अंड ब्रह्मंड खंड भी माटी, माटी नव निधि काया।
माटी खोजत सतगुरु भेट्या, तिन कछु अलख लखाया।
जीवत माटी मूया भी माटी, देखौ ग्यान बिचारी,
अंति कालि माटी मैं बासा, लेटै पांव पसारी,
माटी का चित्र पवन का थंमा, व्यंद संजोगि उपाया।
भानै घड़ै सँवांरै सोई, यहु गोव्यंद की माया।।
माटी का मंदिर ग्यान का दीपक, पवन बाति उजियारा।
तिहि उजियारै सब जग सूझै, कबीर ग्यांन बिचारा।।
(दे. सू. सज्हद 32, पा. उल्लुमा उहिय 21 वही पृ. 587 हसन निजामी की टीका)
हम भी पांहन पूजते, होते रन के रोझ
सतगुरु की किरपा भई, डार्या सिर थैं बोझ।
जिहि हरि की चोरी करी, गये राम गुण भूलि
ते विधना बागुल रचे, रहे अरध मुखि झूलि।
यह मनुष्य के पशु योनि में जाने का इसलाम का मस्ख नामक तनासुख अथवा जन्मान्तरवाद है।
मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता यह इसलामी सिद्धान्त है और कबीर ने इसे बहुधा व्यक्त किया है—
मानिख जनम अवतारा, नां ह्वै है बारंबारा।
मनिषा जनम दुर्लभ है, देह न बारंबार,
तरवर थैं फल झड़ि पड्या, बहुरि न लागै डार।
कबीर हरि की भगति करि, तजि विषया रस चोज,
बार-बार नहिं पाइस, मनिषा जन्म की मौज।
कबीर का कर्मवाद भी मुसलमानी सिद्धान्त के अनुकूल है।
करम करीमां लिखि रह्या, अब कछू लिख्या न जाइ,
मासा घटै न तिल वधै, जो कोटिक करै उपाइ।
बहुरि हम काहि आबहिंगे।
आवन जाना हुक्म तिसैका, हुक्मै बुज्झि समावहिंगे।
जब चूकै पंच धातु की रचना, ऐसे कर्म चुकावहिंगे।
दर्सन छांड़ि भए समदर्सी, एको नाम धियावहिंगे,
जित हम लाए तितही लागे, तैसे करम कमावहिंगे।
हरिजी कृपा करै जौ अपनी, तौ गुरु के सबद कमावहिंगे,
जीवत मरहु मरहु पुनि जावहु पुनरपि जन्म होई।
कहु कबीर जो नाम समाने, सुन्न रह्या लव सोई।
इस पद में कबीर का इस्लामी स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट है। कबीर का पारब्रह्म अल्लाह कर्ता रूप है—
लोका जांनि न भूलौ भाई।
खालिक खलक खलक मैं खालिक सब घट रह्यो समाई
अला एकै नूर उपनाया, ताकी कैसी निन्दा,
ता नूर थैं सब जग कीया, कौन भला कौन मन्दा।
ता अला की गति नहीं जानी, गुरि गुड़ दीया मीठा,
कहै कबीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा।
और यही नहीं सृष्टि का उत्पादन भी उसी कोटिक्रम में है।
कबीर के नारद इबलीस हैं।
चौसठि दीवा जोइ करि, चौदह चंदा माहि-
चौदह चंदा मुसलमानों में पूर्णमासी के लिए आता है।
अवतार के लिए उन्होंने नरसिंघ प्रभू कियौं नहीं लिखा वरन इस दृष्टि से कि अल्लाह कर्ता है, वह किसी रूप में भी उद्धार कर सकता है अतः वे उपाधिवादी हैं।
इस प्रकार मुसलमानी संस्कारों का कबीर में व्याप्त होना दिखायी पड़ता है। यद्यपि वे स्वतंत्र विचार के सूफी यानी जिन्दीक है इसलिए सूफी परंपरा की बातें वे ग्रहण करते हैं, जिससे कट्टर इसलामियत उनमें नहीं मिल पातीं।
उनमें योग मिलता है योग दर्शन के प्रतिपादन के लिए नहीं,वरन काम के अंकुश के लिए।
वे अपने को नामदेव आदि के साथ भक्तों की कोटि में नहीं रखते, गोरख आदि के साथ अभ्यासी की कोटि में रखते हैं।
यों तो चन्द्रबली पांडे जी का मत यह है—
कबीर वास्तव में मुसलमान कुल में उत्पन्न हुए और मुस्लिम संस्कार से बंधे जीव थे जो स्वतंत्र विचार और सत्य के अनुरोध के कारण इस्लाम से आजाद हो गये और धीरे धीरे जिंद से केवल वैष्णव बन गये। किन्तु वे अन्त में यही कहते हैं कि-
“हम तो प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कबीर को जिन्द कहना ही साधु समझते हैं।“
अर्थात उनका ‘वैष्णवत्व’ भी ‘जिन्दीक’ रूप में ही है।
इससे यह विदित होता है कि कबीर की अभिव्यक्ति मुसलमानी ढाल पर ढली हुई है।
उधर कबीर में हमें हठयोग का शास्त्रीय रूप भी दिखायी पड़ जाता है।
हँस न बौलै उनमनीं, चंचल मेल्ह्या मारि,
कहैं कबीर भीतर भिद्या, सतगुरु कै हथियारि।
बिन्दु कबीर की चौहाट है।
चौपड़ि मांडी चौहटै, अरध उरध बाजार
कहै कबीरा रामजन, खेलै संतविचार
सायर नाही, सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाँहि
कबीर मोती नीपजै, सुन्निसिषर गढ़ माँहि
मन लागा उन्मन्न सौं, गगन पहूंचा जाइ
देखा चंद विहूँणा चाँदिणां, तहाँ अलख निरंजन राइ
मन लागा उनमन्न सौं, उनमन मनहिं विलग्ग
लूंड़ विलागा पांणियाँ, पाँणी लूंड़ विलग्ग
गगन गरजि अमृत चवै, कदली कवल प्रकास
तहाँ कबीरा बंदिगी, कै कोई निजादस
कबीर कवल प्रकासिया, ऊग्या निर्मल मूर
निस आँधियारी मिटि गई, जागे अनहद नूर
अनहद बाजै नीझर झरै, उपजै ब्रह्म गियान
अभिमत अंतरि प्रगटै, लागै प्रेस धियान।
अकासे मुखि, औधा कुवाँ, पाताले पनहारि
ताकर पाणी को हंसा पीवै, विरला आदि विचारी
सिव सकती दिसि कौण जु जौवैं, पछिम दिसा उठें धूरि
जल में सिंध जु घर करै, मछली चढ़ै खजूरि
सुरति ढीकुली, लेज ल्यौ, मन चित ढोलन हार
कँवल कुंवा मैं प्रेमरस, पीवै बारंबार
गंग जमुन उर अंतरे, सहज सुंनि ल्यौ घाट
तहाँ कबीरै मठ रच्या, मुनिजन जोवें वाट
इन उल्लेखों से विदित होता है कि कबीर को जितना इस्लाम का ज्ञान था, उससे भी अधिक हठयोग का था। क्योंकि इस्लाम विषयक जितनी बातों का उल्लेख किया है, वे इतनी सामान्य हैं कि उन्हें मुसलमानों के साधारण संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी जान सकता है, पर हठयोग विषयक कबीर के उल्लेख असाधारण ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं। हठयोग के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों का उसने प्रयोग किया है। उस समस्त साधना के एक विस्तृत स्वरूप को उसने प्रस्तुत किया है।
इसी के साथ हम देखते हैं कि नाम का आश्रय प्रबल हैं,वह नाम भी राम का है। इस रामनाम के साथ वैष्णवत्व लगा हुआ है। इसी के साथ भक्ति भी है। कबीर का स्वरूप श्री चन्द्रबली पांडे जी ने यों दिया हैः—
“कबीर की साधना में हठयोग का भी पूरा योग है। कबीर वेदान्त, हठयोग और प्रेम को एक में मिलाकर साधना के क्षेत्र में उतरते और केवल की प्राप्ति करते हैं। कबीर ने हठयोग पर इतना ध्यान दिया है कि लोग उन्हें गोरखनाथ का चेला बना देना चाहते हैं, एवं ब्रह्म तथा केवल का इतना उल्लेख कर दिया कि लोग उन्हें शंकर से अलग नहीं देख सकते, रही प्रेमभगति की साखी सो वह उन्हें वैष्णव बनाने के लिए तुली हैं। कबीर अपने को वैष्णव तो नहीं पर वैष्णव को अपना साथी अवश्य समझते हैं। आखिर बात है क्या कि कबीर वेदान्ती, योगी और वैष्णव दिखायी तो दे जाते हैं, परन्तु अपने को समझते सदैव उनसे भिन्न हैं।“ (विचार विमर्श पृ. 32)
इसके साथ यह भी जोड़ना पड़ेगा कि वे ‘कुरान और इस्लाम’ के अनुयायी जैसे भी लगते हैं, पर हैं नहीं, ‘पांडे जी’ का निष्कर्ष है। ऐसा इसलिए है कि वे सूफी हैं, जिन्द हैं, स्वतंत्र विचार के मुसलमान है। पर प्रश्न है कि क्या यह इतना ही यथार्थ है? कबीर के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए कसौटी क्या होनी चाहिए? यहि हाँ तो कबीर के निर्माण के तत्व क्या ये हैं? कि-
1. उन्होंने गोवध का विरोध किया।
2. उन्होंने अपने को ‘कोरी’ अथवा जुलाहा लिखा है।
3. उन्होंने लिखा है ‘चौथे पन में जन का ज्यंद’
4. उन्होंने अपनी ‘हज’ गोमती तीर पर पीताम्बर पीर के यहाँ बतायी।
5. उनकी कुछ रचनाओं में कुरान तथा सूफी कवियों की छाया मिलती है।
6. वे मनुष्य का पुनः मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करने के सिद्धान्त को नहीं मानते।
7. उनके ‘कर्म’ का स्वरूप कुछ और है?
8. ‘पूरब जनम’ का उल्लेख प्रकृति-विधान अथवा ‘लौह महफूज़’ के लिए है।
9. वेद और कुरान का जहाँ विरोध किया है वहाँ यह भी लिखा है ‘वेद कतेब कहौ क्यूं झूठा, जो न बिचारें’
10. वे ‘जोति’ से सबको उत्पन्न मानते हैं।
11. उनका उद्देश्य प्रेम का प्रचार था।
12. उन्होंने चौदह चंदा पूर्णिमा को लिखा हैं।
13. उन्होंने हठयोग की साधना का वर्णन किया है। कुण्डलिनी, सुरति, निरति, चक्र, इड़ा-पिंगला, सुषुम्ना का उल्लेख उन्होंने किया है।
14. राम के नाम का जाप और भक्ति का उन्होंने प्रतिपादन किया है।
15. उन्होंने राम को अवतार के रूप में भी माना है, और यह भी लिखा है कि ‘ना दशरथ घर औतरि आया’।
16. उन्होंने ‘मरजीवा’ बनने का आदेश दिया है।
17. कबीर ने ‘गुर’ का महत्व माना है, और उसे ‘गोविंद’ से भी बढ़कर स्वीकार किया है—
‘गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागूं पाँव
बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताय’
18.’संत’ के स्वरूप को उन्होंने महत्व दिया है---उसे सारग्राही बताया है—
‘सार सार को गहि रहे थोथा देइ उड़ाय’
19. उन्होंने माया के अस्तित्व को स्वीकार किया है, पर उसे ठगिनी माना है---
‘माया महा ठगिनि हम जानी’
20. उन्होंने ‘मस्जिद’ और ‘मन्दिर’ दोनों का विरोध किया है।
21. उन्होंने न हिन्दुओं को ठीक मार्ग पर पाया न मुसलमानों को
‘हिन्दुन की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई’
कबीर के इस समस्त स्वरूप को दृष्टि पथ में लाते ही यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि कबीर को किसी एक संप्रदाय या मज़हब का, अथवा उससे प्रभावित नही मान सकते। कबीर बे पढ़े थे। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह लोक ज्ञान था अतः लोक-धर्म ही कबीर ने प्रस्तुत किया। लोक धर्म ही वस्तुतः सारग्राही हो सकता है। लोक धर्म का सार ग्रंथों से नहीं लोकवार्ता से ग्रहण किया जाता है। कबीर से पूर्व के विविध संप्रदायों में प्रचलित विविध बातें लोक धरातल पर पहुँच कर लोक-धर्म का सारग्राही रूप प्रस्तुत कर रही थीं, उसी लोग-धर्म को कबीर ने अपनाया, उसी को उसने हिन्दू मुसलमानों की कसौटी माना। उसी को उसने साहित्य में अपने शब्दों और साखियों द्वारा उतार दिया। इस लोक-धर्म में विविध संप्रदायों की गहरी बातें भी किसी सीमा तक ग्रहण कर ली गयी थीं पर वे सभी ऐसी बातें थीं जिनमें परस्पर संप्रदाय भावना का आग्रह नहीं था। उनमें एक समन्वय और सामञ्जस्य था। वह समन्वय और सामञ्जस्य लोकवार्ता के क्षेत्र में साधारणीकृत हो गया था।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.