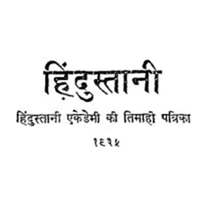सन्तरण कृत गुरु नानक विजय - जयभगवान गोयल
रोचक तथ्य
Santran kart Guru Nanak vijay, Anka-1-2, 1970
गुरु नानक विजय 24382 छंदों का एक धर्मप्रधान वृहदाकर प्रबन्ध काव्य है। जिसका प्रणयन उदासी सम्प्रदाय के प्रमुख कवि संतरेण ने 19वीं शती के उत्तरार्ध में किया था।
उत्तर भारत का मध्ययुगीन भक्ति-आंदोलन अनेक मतों-सम्प्रदायों एवं पंथों के माध्यम से विकसित हुआ। उदासी सम्प्रदाय भी इसी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक अंग है। इस सम्प्रदाय का संगठन अभी भी बहुत मजबूत है। चार धूणी, 6 बख्शीशी एवं अनेक उपबख्शीशी के रूप में अनेक स्थानों पर इनके बड़े आश्रय अखाड़े है। गुरु नानक के ज्येष्ठ गुरु बाबा श्रीचंद को इस पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। इस सम्प्रदाय के वर्तमान प्रमुख आचार्य एवं संत श्री गंगेश्वरानंद जी की मान्यता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी इस सम्प्रदाय के आदि आचार्य थे। इनके प्रशिष्य श्री सर्वज्ञ मुनि जी के अनुसार श्रीचंद जी गुरु-गद्दी की 108 वीं नानक विजय में उन्होंने गुरु नानक का उदासी भेषधारी, भगवान के अवतार के रूप में निष्ठापूर्वक वर्णन किया है।
संतरेण का जीवन-वृत्त
संतरेण के जन्म के संबंध में निश्चित रूप से तो कुछ मालूम नहीं लेकिन अनुमान है कि उनका जन्म संवत् 1798 में श्रीनगर, कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिबल्लभ और माता का नाम सावित्री देवी था। ये गौड़वंशीय ब्राह्मण थे। इन्होंने संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। बाद में बाबा साहिबदास से शिक्षा लेकर उदासी सम्प्रदाय में प्रवेश किया और उन्हीं से वेदान्त, इतिहास, पुराण, काव्य-शास्त्र एवं काव्य-रचना का ज्ञान प्राप्त किया। यह भी कहा जाता है कि इन्होंने लाहौर, मालवा, सिंध, अकीला एवं मद्रास आदि स्थानों की यात्राएँ कीं तथा अनेक अखाड़ों और पीठों की स्थापना की। फाल्गुन बदी 12 संवत् 1932 को मालेर कोटला के निकट भूदन ग्राम (पंजाब) में इनका देहावसान हुआ जहाँ अभी इनकी समाधि है। संतरेण बड़े ही प्रतिभाशाली विद्वान् एवं निष्ठावान साधक थे। वे एक समन्वयवादी चिंतक, सच्चे संत, समाज सुधारक एवं धर्म प्रवर्तक थे और उनका व्यक्तित्व विनयशील, निराभिमानी एवं प्रभावशाली था।
गुरु नानक विजय
उदासी बोध में इन्होंने नानक विजय, मनप्रबोध, वचनसंग्रह तथा नानक बोध इन चारों रचनाओं का उल्लेख किया है। नानक विजय संतरेण की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 20 खंड, 347 अध्याय तथा कुल 24382 छंद है। खण्डों के नाम हैं- मंगल खण्ड, ब्रह्म खण्ड, नानक विलास खण्ड, धर्म उद्योग खण्ड, बियाह खण्ड, उदासी खण्ड, प्रताप खण्ड, खडूर खण्ड, मकेश्वर खण्ड, सुमेर खण्ड, रोमेश्वर खण्ड, गिआन खण्ड, नानक खण्ड, कश्मीर खण्ड और करतारपुर खण्ड। ये नाम स्थानों, घटनाओं एवं विषय वस्तु पर आधारित है। इस ग्रंथ में इसके रचनाकाल का उल्लेख नहीं है। संवत् 1926 में रचित उदासी-बोध में इसका उल्लेख है, लेकिन भाई संतरेण सिंह के संवत् 1880 में रचित नानक प्रकाश तथा 1900 में रचित गुरु प्रताप सूरज में इसका उल्लेख नहीं है। इससे विदित होता है कि इस ग्रंथ की रचना 1910 वि. के आसपास हुई। यह ग्रंथ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ (गुरुमुखी लिपि में) संतरेण आश्रय भूदान, बालापुर पीठ, अकोला तथा साधु-बेला आश्रम, सक्खर में उपलब्ध है।
कथा-तत्व
गुरु नानक विजय में गुरु नानक के जीवन का अत्यंत विस्तृत, विशद् एवं चमत्कारित वर्णन हुआ है। इनके पिता कालू का विवाह, इनके जन्म, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के कार्यों, विवाह, यात्राओं धर्म-प्रचार एवं लहना को गुरु-गद्दी देकर ज्योति-ज्योति समाने आदि का निष्ठापूर्वक वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना वाल्मीकि ऋषि से भेंट होने पर उनके प्रोत्साहन एवं आकाशवाणी से प्रेरणा पाकर की गई। कवि के अनुसार यह कथा सभी फलों को देने वाली एवं अत्यन्त पवित्र है।
मूलरूप में यह एक धार्मिक काव्य-ग्रन्थ है, जिसमें गुरु नानक के चरित्र को पौराणिक रूप देकर प्रस्तुत किया गया है। मध्ययुग में प्रायः सभी सम्प्रदायों ने अपने मत के प्रचार के लिए कथा-काव्यों का आश्रय लिया है, उन्होंने अपने सिद्धान्तों का निरूपण भी किया है और अपने ध्रम संस्थापकों की महिमा-मंडित प्रशंसा भी। उनके चरित्र में अतिमानवीय एवं चमत्कारपूर्ण तत्वों का समावेश करके उन्हें अलौकिक रूप प्रदान किया गया है। उनके जीवन की छोटी से छोटी और साधारण से साधारण घटना को भी विचित्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। नानक विजय में भी मध्ययुगीन धर्म-भावना का प्रसार सर्वत्र देखा जा सकता है। इसमें भी यथार्थता कम और कल्पना का उन्मेष अधिक है तथा इतिहास को पृथक् रूप दिया गया है। इसमें पारलौकिक दृश्यों अतिमानवीय कृत्यों एव चमत्कारपूर्ण घटनाओं का बाहुल्य है। चरित्र नायक की महानता और दिव्यता प्रदर्शित करने के लिए कथानक में अनेक अलौकिक एवं विस्मयजनक घटनाओं का समावेश किया गया है और ऐतिहासिक घटनाओं में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन-परिवर्धन कर दिया गया है। वस्तुतः कथानक तो एक माध्यम है, लेखक का उद्देश्य है कथा से अनपे सिद्धान्तों का निरूपण और उदासी मत के उद्धारक (संतरेण के अनुसार) गुरु नानक की महिमा का वर्णन। इस ग्रन्थ में व्याप्त पौराणिक-तत्व को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इसे नवपुराण की संज्ञा भी दी है।
धार्मिक प्रवृत्ति का आभास ग्रन्थ के आरंभ में ही मिल जाता है। प्रारंभिक 16 अध्यायों में गणेश, राम, कृष्ण नानक तथा उनके पुत्रों, विष्णु के 24 अवतारों, सिक्ख गुरुओं उदासी सम्प्रदाय के चार धूणों के संस्थापकों, सन्तों, ऋषियों, कवियों, देवी-देवताओं एवं विप्रों आदि की वन्दना संबन्धी मंगलाचरण है। तदनन्तर पौराणिक पद्धति का अनुकरण करते हुए पूरे धार्मिक वातावरण में महाविष्णु द्वारा नानक रूप में अवतार लेने के कारणों के उपाख्यान से कथा का आरम्भ होता है। भगवान के नानक रूप अवतरित होने के तीन प्रमुख कारणों का उल्लेख किया गया है। (1) जनक की प्रार्थना पर मृत्युलोक के पापियों के उद्धार हेतु (2) कश्यप और अदिति के तप के प्रसन्न होकर पुत्र रूप में उनके यहां जन्म लेने के लिये तथा (3) यवनौं के गौ, ब्राह्मणों पर किये गये अत्याचारों से आतंकित पृथ्वी के उद्धार के लिये। सुक्खासिंह ने गुरु विलास में गुरु गोबिन्दसिंह के अवतार के संदर्भ में अंतिम कारण का उल्लेख किया है। इस दोनों रचनाओं का मुख्य उद्देश्य दैवी-शक्तियों की आसुरी शक्तियों पर विजय दिख़ाना है। लेकिन दोनों का स्वरूप भिन्न है। गुरु विलास का नायक धर्म गुरु होते हुए भी युद्धवीर है और आसुरी शक्तियों के विध्वंस के लिए खड्ग धारण करता है, जबकि नानक विजय का नायक केवल धर्म-प्रचार द्वारा ही उन पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए गुरु विलास वीररस प्रधान रचना है और नानक विजय शान्तरस प्रधान। कश्यप की तपस्या का उल्लेख भाई संतोख सिंह ने नानक प्रकाश में भी किया है। ऐसा चरित्र नायक को पौराणिक रूप देने के लिये ही किया गया है। नानक विजय में भगवान सब देवताओं तथा योगमाया आदि को भी अवतार लेने का अंदेश देते हैं। ब्रह्मा कालू के कुल पुरोहित हरिदयाल के रूप में अवतरित हुए हैं। सभी देवता कालू के सेवक बने हुए हैं, सुलक्षणी योगमाया है, नानकी मीरा की और उसके पति जयराम गिरधर के अवतार है।
वर-कथाओं की तरह यहाँ शाप-कथाएँ भी हैं। नारद भगवान् के शाप के परिणाम स्वरूप ही मिरासी मरदाने के रूप में अवतरित हुए है।
गुरु नानक का जन्म भी मिशन वातावरण में ही होता है। वे चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर माता को दर्शन देते है और फिर सोहं का उच्चारण करके बालक का रूप धारण कर लेते है। शैशवावस्था में ही वे ब्राह्मणों को वेदों-उपनिषदों का ज्ञान देने लगते हैं। और जब गोरखनाथ दर्शनार्थ आते हैं तो विराट् रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। उनके माता-पित, सखा-सेवक, राजा-प्रजा, नाथ-सिद्ध आदि सभी उन्हें भगवान का अवतार मानते है। वे सभी को अपनी अलौकिक शक्ति से बिस्मित एवं प्रभावित करते दिखाये गये है।
नानक यहाँ इतिहास-पुरुष नहीं, पौराणिक पुरुष हैं और उनके अतिमानवीय कृत्यों एवं करामतों से यह ग्रन्थ भरा पड़ा है। दो वर्ष की अवस्था से ही भारी नामक ठग के उद्धार से उनके चमत्कारिक कृत्यों का आरम्भ हो जाता है। फिर तो वे अन्धों को आँखें देते हैं, कोढ़ियों को रोग मुक्त करते है। और मृतकों को जीवित करते हैं। उनके कथन मात्र से लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, स्पर्श मात्र से राक्षस दिव्य रूप धारण कर लेते है, दौलत खाँ लोदी का कुत्ता भी उनके हाथ फेरने से कुरान पढ़ने लगता है। किसी की बे जबान बन्द कर देते है। तो किसी (काज़ी) को जमीन से चिपका देते हैं। खेत को गायों से चरवा देने पर भी हरा-भरा रहता है, मोदी खाने के संतों को लुटवा दिये जाने पर भी वह भरा-पूरा रहता है। एक स्थान (तलवंडी) से अदृश्य होकर अन्यत्र (कुरुक्षेत्र) में पहुँच जाते हैं। सूक्ष्म शरीर धारण करके पर्वतों को लाँघ जाते है। उनका सुलक्षणी को दिया हुआ श्रीफल बालक का रूप धारण करके (श्रीचंद) 5 वर्ष के बालक की तरह खेलने लगता है। लक्ष्मीचंद भी एक लौंग से बन जाता है। वे अनेक रूप धारण कर लेते हैं, पत्थरों को चाँदी के रूप में बदल देते हैं, रोटी निचोड़ कर उसमें से खून अथवा दूध निकाल देते हैं और इब्राहिम लोदी के राज्य के विनाश की भविष्यवाणी कर देते हैं।
वे अपने अलौकिक शक्ति से स्वर्ग लोक, पातालस सचुखंड महाविष्णु लोक, बैकुंठ आदि का भ्रमण करते हैं, गोरखनाथ, वरुण, ध्रुव भक्त आदि से भेंट करते हैं। विष्णु से अपनी पूजा करवाते हैं और जल में अन्तर्निहित होकर भगवान के पास पहुँच जाते हैं।
यहाँ माया-नगरियाँ हैं, ज्वाला स्वरूपा नारियाँ है, सोने के वृक्ष, सोने की लताएँ है और अमृत के फूल है। भगावन स्वयं बाला के रूप में, मोदीखाने में नानक की सहायता करने आते है।
इस तरह सम्पूर्ण कथानक लौकिकता और यथार्थ के धरातल से ऊपर उठकर अलौकिक एवं रहस्यमय रूप धारण किये हुए है। इसमें स्वाभाविकता के स्थान पर अतिमानवीयता एवं वैचित्र्य अधिक है। सभी पात्रों को नानक के अबतारत्व का बोध निरन्तर रहता है, जो कथानक के स्वाभाविक विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। यहाँ पात्रों के पूर्व जन्म की कथाएँ भी हैं, अवतार कथाओं के रूप में भयंकार बंदर, हेमपुरी, अंधेरनगरी, अंगददेश, हरिद्वार आदि की कथाएँ भी आई है। और नारद के मोह-भंग आदि से सम्बद्ध पौराणिक आख्यान भी हैं। ऐतिहासिक घटनाओं पर पौराणिक रंग चढ़ाने का कवि को इस कदर मोह है कि उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहता कि इससे राष्ट्रीय भावना को कितनी क्षति पहुँचती है। उदाहरण के लिये, यहाँ बाबर को अत्याचारी इब्राहीम को दण्डित करने के लिए नानक वाणी की प्रेरणा से ही भारत पर आक्रमण करते दिखाया गया है। इस तरह हम देखते है कि इस ग्रंथ में या तो नानक की कारामातों का वर्णन अधिक है या उनकी धर्म-यात्राओं और उपदेशों का। भगवान् से आशीर्वाद पाकर उदासी वेश धारण करके वे धर्म-यात्रा पर निकल पड़ते है। सुल्तानपुर से उनकी धर्म विजय का शुभारंभ होता है। पहला उपदेश मानवीय एकता तथा संसार की निरर्थकता एवं असारता का अपनी बहन नानकी को देते है फिर अपनी चार उदारसियों में पानीपत दिल्ली, लाहौर कुरुक्षेत्र बीकानेर अंचल तीर्थ, गुजरात, पुष्कर, जयपुर, उज्जैन, चांगदेश, पंचवटी, पढरपुर, मानसरोवर, सुमेर पर्वत, अंगददेश लंका, रामेश्वरमू, नानकमता, सूर्यकुंड, काशी, कौरुदेश, संगलदीप, बशहर देश, विश्वेसपुर, देवगंधार, पाकपटन, गिरनार पर्वत, मक्का, काश्मीर, तथा विष्णुलोक, सचुखंड, महाविष्णु लोक आदि स्थानों का भ्रमण करते हैं। विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थानों और तीर्थों पर जाते हैं, वहाँ उन धर्मों-मतों के धर्म-गुरुओं, पंडितों, महन्तों, पीरों-फकीरों आदि से धर्म-चर्चा करते है, सेठों, साहुकारों, सुलतानों और राजाओं को उपदेश देते है तथा दीन-दुखियों, रोगियों एवं पापियों का उद्धार करते हैं।
पीर-फक़ीर, साधु-संत, योगी-जंगम, सिद्ध-महन्त, शेख-ब्राह्मण, शैव-शाक्त, हाजी-काजी, मुल्ला-इमा, जैनी-वैष्णव सभी उनसे चकित, प्रभावित एवं पराजित होकर उनके शिष्य बनते दिखाये गये हैं। वस्तुतः इस ग्रन्थ की समस्त कथावस्तु में धार्मिक तत्व की ही प्रधानता है। बहुत से प्रसंगों में इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप वार्ता की सी निरसात, उपदेशात्मकता, एवं एकता आ गई है। आरम्भिक कथा में कुछ सन्तुलन है लेकिन बाद के कथानक में धर्म-प्रचार एवं सिद्धान्त-निरूपण की अतिशयता के कारण कथानक का सूत्र ढीला पड़ जाता है। उसमें उपदेशों की शुष्कता, पारलौकिक दृष्यों का वैचित्र्य, करामातों का कौतुक अधिक है और जीवन की यथार्थता एवं रसात्मकता अपेक्षाकृत कम। इसमें घटनाओं का बाहुल्य है और वर्णनों में इतवृत्तात्मकता है। पौराणिक आख्यानों का नियोजन यद्यपि इतनी कुशलता से किया गया है कि वे मूल कथा के अंग लगते हैं, तथापि कथानक में धार्मिक प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि न तो कथा का स्वाभाविक विकास हो पाता है और न ही युग का व्यापक एवं विशद् चित्र उभर कर सामने आता है। युग-दशा की नाम पर उस युग में प्रचलित विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों-पन्थों के स्वरूप, विकृत साधना पद्धतियों एवं बाह्याचारों का ही उल्लेख अधिक मिलता है। इससे कुछ वर्ष पूर्व रचित गुरु प्रताप सूरज में युग और समाज का जैसा वृहद् और यथार्थ चित्र उपलब्ध है, उसका यहाँ प्रभाव है। पात्रों की मनोदशा का वैसा सजीव चित्रण भी यहाँ नहीं हुआ और न ही भावों की वैसी विशद और अनुभूतिपूर्ण अभिव्यंजना हुई है। सभी पात्र नाटक की दिव्यता से को बोध से इनते दबे हुए हैं कि उनकी मानवीय मनोवृत्ति एवं संवेदना पूरी तरह उभर कर सामने नहीं आ पाती।
सन्तरेण ने आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता में विश्वास प्रकट किया है (वि. ख. 21।31)। आत्मा को उन्होंने सच्चिदानन्द स्वरूप माना है, जो न मरता है, न जन्म लेता है। वह अविनाशी और चेतन रूप है। यह शरीर अनित्य, रोगयुक्त, दुखात्मक, जड़रुप, एवं नाशवान है। परमात्मा के सगुण रूप के प्रति भी सन्तरेण ने आस्था व्यक्त की है। जोकि भक्ति के वश में होकर तथा लीलार्थ अवतार धारण करता है। उनके अनुसार इस मायरूप नामकरूकात्मक, जड़ जगत की उत्पत्ति ब्रह्मक अहं ब्रह्म की ध्वनि से हुई है। यह संसार नाशवान् क्षणभंगुर, अनित्य एवं स्वप्नवत मिथ्या है। संसार के सभी सम्बन्ध, धन, सम्पत्ति परिवार आदि मिथ्या और नश्वर है। सत्य केवल ब्रह्म है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। सभी उसी से उत्पन्न होते है और उसी में लीन हो जाते है।
आवागमन और कर्मफल में भी सन्तरेण को विश्वास है। उनका कथन है कि आवागमन से मुक्ति ज्ञान द्वारा सम्भव है और ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु अज्ञान का विनाशक, भक्ति-मुक्ति को देने वाला और ब्रह्म से मिलाने वाला है। वही दुष्कर्मों से भी मुक्त करता है। सन्तरेण ने भी अन्य सन्तों की भाँति गुरु को परब्रह्म स्वरूप माना है। और उनकी निष्ठापूर्वक वन्दना की है। उनके अनुसार गुरु ही पाप, ताप, क्लेश को मिटा कर हृदय में ज्ञान का प्रकाश करता है। गुरु के बिना न कर्म सार्थक है, न भक्ति मिलती है, न ज्ञान। गुरु के बिना जीव चौरासी योनियों में भटकता है। और वह प्रियतम को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। सच तो यह है कि गुरु के समान और कोई हितकारी ही नहीं है।
आध्यात्मिक तत्व
संतरेण पहले संत एवं धर्म-प्रचारक हैं, फिर कवि। उनकी काव्य रचना का मूल उद्देश्य मन को कुवृत्तियों से मुक्त एवं सांसरिक मोह-माया से विमुख करके उसमें उदात्त-भावनाओं का उन्मेष करना और भगवान के भजन में लगाना है। वे उदासी-सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य एवं साधक थे और इस ग्रंथ में भी उन्होंने इसी सम्प्रदाय के अनुरूप ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि के स्वरूप एवं सम्बन्ध साधना-पद्धति, तथा साम्प्रदायिक आदर्शों और मान्यताओं, गुरु के महत्व, नाम-महिमा, कर्म-फल, आवागमन, संत महिमा, वेदों एवं पुराणों के महत्व, ज्ञान एवं भक्ति, सत्य, संयम, संतोष आदि का निरूपण विस्तार से किया है।
श्री गंगेश्वरानन्द जी ने उदासी शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, उद ब्रह्म, आसीम स्थित। अर्थात् जो ब्रह्म में स्थित हो अथवा ब्रह्मरूप हो। आरम्भ में अन्य संतमतों की भाँति यह मत भी निर्गुणवादी था, लेकिन धीरे-धीरे इसमें सगुणोपासना का प्रवेश होता गया और अब यह पूर्णतः सनातन धर्म का ही एक अंग सा बन गया है, जिसमें वेदों, उपनिषदों के ज्ञान की निष्ठापूर्वक चर्चा की जाती है, पुराणों की कथाएँ सुनाई जाती हैं और पंचदेवोपासना (ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, गौरी) का विधान है। गुरु नानक विजय में भी निर्गुण एवं सगुणोपासना के समन्वय का प्रतिपादन हुआ है और नानक को भी विष्णु के अवतार के रूप में राम और कृष्ण से अभिन्न माना गया है।
संतरेण के अनुसार ब्रह्म निर्गुण, निरंजन, अलख, अभेव, अंतरयामी, अविनाशी रूपरेख रहित, वर्णचिन्ह विहीन, अनाम भी है और सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान भी। उन्होंने उसे अन्य संतों की भाँति राम, रहीम, परम पुरुष, साहब, ब्रह्म, पारब्रह्म, परमेश्वर आदि कई नामों से अभिहित किया है। संतरेण ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं विविध अवतारों को पारब्रह्म रूपी जल से उत्पन्न और उसी में विलीन हो जाने वाली लहरों अथवा तरंगों के समान कहा है। संतरेण ने भक्ति के साथ-साथ ज्ञान, शुभ कर्म, विरक्ति एवं अन्य उपासना-पद्धतियों के महत्व का भी निरूपण किया है, लेकिन प्रमुख भक्ति का ही माना है। उनका मत है कि भक्ति के बिना जीव आवागमन से मुक्त नहीं होता और भव-फाँसी नहीं कटती। भक्ति बिना जप, तप, पुण्य, दान, सब व्यर्थ है। भक्ति बिना शांति भी प्राप्त नहीं होती। भक्ति से ही ज्ञान, वैराग्य, योग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और ब्रह्म से मिलन होता है। उन्होंने निष्काम भक्ति पर अधिक बल दिया और उसके लिए विषय-वासनाओं का त्याग अनिवार्य माना है। क्योंकि वासनायें जीव को बंधन में बाँध रहती है। भगवत्-भक्ति के साथ ही कवि ने संत, ब्राह्मण आदि की भक्ति का भी महत्व दर्शाया है। संत को भी वे ब्रह्म-रूप मानते हैं। संतों के शरीर में, चरण में, वचनों में राम का निवास होता है।
उन्होंने विप्र-पूजा, धर्म-ग्रंथों के अध्ययन, भगवत-कथा, उपवास, व्रत, मूर्तिपूजा, श्राद्ध एवं शकुन विचार आदि में भी आस्था प्रकट की है और जीवहिंसा का विरोध किया है। वर्ण-व्यवस्था में भी उनकी कुछ निष्ठा थी लेकिन भक्ति के क्षेत्र में वे ऊँच-नीच अन्तरि नहिं कोई। हरि को भजेसु हरि का होई, के सिद्धान्त के समर्थक थे। यहाँ वे राम, कृष्ण, गणेश, देवी-देवताओं की वन्दना करते हैं। नानक यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं, जन्मोत्सव पर भी विप्र मौजूद हैं और विवाह-मंडप में भी विप्र वेदमन्त्रों का पाठ करते हैं। जनवासे में पुराणों की कथा होती है। ऐमनाबाद में स्वयं नानक पुराणों की कथा लोगों को सुनाते है। नानक महाविष्णु के और अन्य पात्र नारद, ब्रह्म, देवताओं आदि के अवतार है। वस्तुतः गुरु नानक विजय में कवि वैष्णव मत की ओऱ काफी मात्रा में झुकता दिखाई पड़ता है और कहीं-कहीं मूर्तिपूजा और उपवासों तक का समर्थन करता पाया जाता है। यहाँ स्वयं भगवान यह भी कहते पाए जाते है कि मैं कालू के याहँ जन्म लूँगा, कालू का वश वहीं रघुवंश है जिसमें मैंने रामावतार लिया था। अर्थात् यहाँ कवि नानकावतार और रामावतार की अभिन्नता की घोषणा करता है। ब्राह्मणवाद का इस रचना में अत्यधिक प्रभाव लक्षित होता है। विप्र पूजा एवं विप्र रक्षा का विधान विशेष रूप से किया गया है। वैष्णवों के साथ समन्वय का यह एक सचेष्ट प्रयत्न भी कहा जा सकता है।
लेखक का कथन है कि गुरु नानक ने उदासीवेश धारण करके इस पंथ को अन्य पंथों का शिरोमणि बनाया। नानक यहाँ यह कहते भी पाए जाते है कि उनका पुत्र श्रीचन्द उदासी पंथ को उजागर करेगा और वे स्वयं गुरुदित्ता (श्रीचन्द के शिष्य) के रूप में अवतरित होंगे। गुरु नानक के अतिरिक्त अन्य नौ सिख-गुरूओं की भी इस ग्रंथ में वन्दना की गई है। और गुरु ग्रन्थ साहब को पंचमवेद कहा गया है। इस तरह कवि ने सिख मत के साथ भी उदासीपंथ का सीधा सम्बन्ध स्थापित किया है। इसी प्रकार सन्तरेण ने नाथमत का भी पर्याप्त प्रभाव ग्रहण किया है। सुलक्षणी को दिए गए जिस श्रीफल से इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य बाबा श्रीचन्द की उत्पत्ति होती है उसमें गोरखनाथ का अंश प्रविष्ट होते दिखाया गया है, अर्थात् उन्हें गोरख का अंशावतार बताकर कवि ने उदासी पन्थ और नाथमत का समन्वय स्थापित किया है। नानक को भी नाथ-साधना के अनुरूप नौ द्वारों को पार करके दसवें द्वार में प्रविष्ट होकर भगवान के शून्य रूप में दर्शन करते दिखाया गया है। वस्तुतः मध्ययुगीन धर्म-साधना पर नाथमत का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। सूफी प्रेमाख्यानों में भी प्रायः सभी साधक कथा-नायक अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए योगी बनकर निकलते है।
सन्तरण ने उदासी-पंथ के प्रवर आचार्य होते हुए भी वैष्णवों, नाथों एवं सिक्खों से समन्वय का स्तुत्य प्रयत्न किया है। समन्वय की यह प्रवृत्ति भी गुरुमुखी लिपि में रचित समस्त हिन्दी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। मध्ययुगीन प्रायः सभी सिख-कवियों ने भी सिखमत के वैष्णवों के साथ का महत्वपूर्ण कार्य किया है।
मध्ययुगीन निर्गुण भक्त कवियों (सन्तों) की भाँति सन्तरेण ने भी अपनी साधना में नाम-स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनका मत है कि यन्त्र, मन्त्र, नाम, पुण्य, यज्ञ, तप आदि का भी महत्व है लेकिन नाम सबसे ऊपर है। उसमें विष्णु से भी सौ गुनी शक्ति है। नाम-स्मरण से भव-बन्धन टूट जाते है, यम अधीन हो जाता है, इस लोक में सुख और परलोक में यश मिलता है। और सभी पापों का मैल धुल जाता है। नाम नामी से भिन्न नहीं है, दोनों एक रूप हैं, दोनों महान् हैं, दोनों अविनाशी है। नाम करोड़ों सत्संगों के समान है। प्रेम सहित नाम स्मरण से क्लेशों का समूह नष्ट हो जाता है और मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है।
इस प्रकार हम देखते है कि गुरु नानक विजय में धार्मिक भावना, आध्यात्मिक विचारों, चमत्कारपूर्ण आख्यानों आदि की इतनी प्रधानता है कि यदि इन प्रसंगों को अलग कर दिया जाय तो ग्रन्थ का कलेवर बहुत छोटा रह जायगा। फिर भी वस्तु-वर्णन एवं भाव-व्यंजना सम्बन्धी कुछ स्थल इस ग्रन्थ में ऐसे हैं, जिनमें यथेष्ट रसात्मकता और कवि की काव्य-प्रतिभा का प्रकाश है।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.