कबीर द्वारा प्रयुक्त कुछ गूढ़ तथा अप्रचलित शब्द पारसनाथ तिवारी
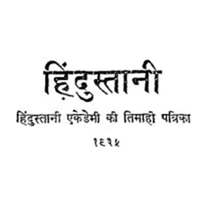
कबीर द्वारा प्रयुक्त कुछ गूढ़ तथा अप्रचलित शब्द पारसनाथ तिवारी
हिंदुस्तानी पत्रिका
MORE BYहिंदुस्तानी पत्रिका
मध्यकाल के प्रायः सभी प्रमुख हिन्दी-कवियों ने ऐसे अनेक सभ्द अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किये हैं जो उस समय तो जनता में प्रचलित रहे होंगे, किन्तु आज उनका प्रचलन कम होने के कारण और कोशों में भी अधिकांश का उल्लेख न होने के कारण उनके टीकाकारों को प्राय भ्रम हो जाया करता है। प्रस्तुत निबन्ध में कबीर द्वारा प्रयुक्त कतिपय ऐसे ही शब्दों के उपयुक्त अर्थ ढूँढ़ने का प्रयास किया गया है। ये सभी शब्द उनके पदों से लिये गये हैं और स्थल-निर्देश हिन्दी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय, द्वारा प्रकाशित कबीर-ग्रन्थावली के अनुसार है। विवेच्य शब्द क्रमशः निम्नलिखित है।
(1) गिलारि
पद 26-10 खंभा तैं प्रगट्यौ गिलारि। हिरनांक्रस भारयौ नख बिदारि। ना. प्र. सभा द्वारा प्रकाशित कबीर-ग्रन्थावली के एक टीकाकार श्री पुष्पपाल सिंह ने उपर्युक्त पंक्ति की जो टीका दी है उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने गिलारि का नृसिंह अर्थ ग्रहण किया है। किन्तु यह अर्थ अनुमानजनित है, यह आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जाएगा। इस शब्द के पाठान्तरों से ज्ञात होता है कि बहुत पहले ही लोग इसके ठीक अर्थ से अनभिज्ञ होने के कारण इससे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। कबीर चौरा से प्रकाशित शब्दावली में इसका पाठान्तर मुरारि मिलता है। गुरु ग्रन्थसाहब में उपर्युक्त पंक्ति का पाठ इस रूप में मिलता हैः प्रभु थंभ तें निकसे करि बिसथारु। किन्तु पाठ निर्धारण का यह एक मान्य सिद्धांत है कि प्रायः अनगढ़ और क्लिष्टतर रूप प्राचीनतर सिद्ध होते हैं- भले ही उनका अर्थ हम सरलता से न समझ पाएँ। मैंने कबीरवाणी का पाठ-निर्णय करते समय इसी सिद्धान्त के अनुसार गिलारि पाठ ग्रहण कर लिया, किन्तु उसके उपयुक्त अर्थ की चिन्ता भी स्वाभाविक थी। इस शब्द के उचित अर्था का समाधान बखना वाणी के एक पंक्ति से हो सकता है, जो इस प्रकार है- थंभा मांहि पिलारया। तैं जन प्रहलाद। स्वामी मगलदास सम्पादित, पद 16.5)
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि कबीर-ग्रन्थावली का गिलारि (-गरज कर) क्रियापद है, न कि संज्ञापद, जैसा कि उसके उपर्युक्त टीकाकार से समझा है। स्वामी मगलदासजी ने बखना-वाणी की टिप्प्णी में गिलारया का अर्थ दिया हैः गर्जना की, और यही अर्थ इस प्रसंग में उपयुक्त भी लगता है। फिर भी इसकी व्युत्पत्ति की समस्या कदाचित् असंगत न होगा कि प्रह्लाद सम्बन्धी समान प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग सम्भवतः उन्होंने कबीर से ही प्रभावित हो कर किया है।
(2) चवै
पद 28.2 हरिजन हंस दसा लिएं डौले। निरमल नाँव चवै जस बोलै।। बीजक में दूसरी पंक्ति का पाठान्तर हैः निरमल नाम चुनोचुनि बोले। चवै का अर्थ पहले स्पष्ट न रहने के कारण मैंने बीजक-पाठ की सहायता से चवै के स्थान पर चुनै रखा था, किन्तु सन्देशरासक (94.2 आलिंगणु अवलोयण चुंबणु चवणु सुरय रसु।) से इसका समुचित अर्थ मिल गया और मुझे कबीर-ग्रंथावली के शुद्धिपत्र में इस परिवर्तन की सूचना देनी पड़ी। यहाँ यह संकेत कर देना आवश्यक है कि कबीर या सन्देशरासक के कर्ता अब्दुल रहमान के चवै या चवणु तुलसी के बिधु बिख चवै स्रबै हिमु आगी। (रामचरित मानस, अयोध्या काण्ड-168) में मिलने वाले चवै के समान चूना या प्रस्रवण के बोधक नहीं हैं, प्रत्युत दोनों ही स्थलों पर वे बोलने के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। (तुल. पाइयअ सद्द महण्णवी चव- बोलना) जिसके समानान्तर प्रयोग मध्यकालीन साहित्य में भी दुर्लभ हैं।
(3) जंबूरै
पद 34-9, जुगति जबूंरै पाइया बिसहर लपटाई। अवधी तथा भोजपुरी में जम्बूरा मदारी के सहायक को कहते हैं, किन्तु इस शब्द की व्युत्पत्ति का कुछ पता नहीं लगता और न तो किसी कोश में ही यह शब्द मिल सका है।
(4) पांन
पद 53.7 जोलहै तनि बुनि पांन न पावल। फारि बिनै दस ठांई हो। कबीर में पान शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक तो मुहावरे के रूप में जैसे साखी 22-7-1 में, पसुवा सौं पांनौं परौ (तुल., आधुनिक मुहावरा-पाला पड़ना)। दूसरे पार अर्थ में जैसे रमैनी 2-2 कोई न पूजै बासों पांनां। अथवा साखी 17-8-2 में- तहां नहीं काल का पांन। (समान प्रयोग के लिए तुलनीय बखान पद 159.1- भोजन क्युं तिरूं रे म्हारी पांन न पूजै कोइ।) और तीसरे बुनाई के धन्धे में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द के रूप में। जुलाहों का पांन क्या है, इसका कुछ अनुमान दादू की इन पंक्तियों से लगाया जा सकता हैः----
प्रेम पाण लगाई धागै तत तेल निज दीया।
एक मनां इस आरंभ लागा ग्यांन राछ भरि लीया।।
इससे यह ज्ञात होता है कि पान सूत में लगाया जाने वाला कोइ पदार्थ है। कबीर वाणी की एक प्राचीन टीका में भी जिसका रचयित अज्ञात है। द. हिंदी अनशीलन वर्ष 13, अंक 34) पान के साथ प्रेम शब्द जोड़ दिया गया है- माया प्रीति नहीं, प्रेम पांन लाई। अन्य टीकाओं से इस स्थल के सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं मिलती। हिन्दी शब्दनागर (पृ. 2076) में सुझाया गया है कि सूत को माड़ी से तर करके ताना करने की क्रिया को जुलाहों की शब्दावली में पांन लगाना कहते है। प्रस्तुत प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग पिछले दोनों अर्थो में हो सकता है- पार पाने के अर्थ में अथवा माड़ी लगाकर सूत का ताना करने के अर्थ में। वयन-व्यवसाय का प्रसंग होने के कारण पिछला अर्छ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।
(5) अहरखि अथवा आहर
पद 65-1, मन रे अहरखि बाद न कीजै। अपनां सुक्रितु भरि भारे लीजै।। जिन प्रतियों में कबीर का यह पद उपलब्ध होता है, सभी में अहरखि पाठ ही है, किंतु इसकी व्यत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसके विभिन्न अर्थ सुझाये है। उदाहरणार्थ, भोजन के लिए (डा. रामकुमार वर्मा, सन्त कबीर, परि. पृ. 132), हिर्स में पड़ कर या दूसरे की देखा देखी (पं. परशुराम चतुर्वेदी, पत्र द्वारा), अहं+रखि अर्थात् गर्वपूर्वक (श्री नरोत्तमदास स्वामी, पत्र द्वारा), अहर्निश (श्री पुष्पपाल सिंह, कबीर-ग्रंथावली सटीक, पृ. 353) आदि। किन्तु इन सुझावों के आधार क्या है यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता। इसीलिए मैंने कबीरग्रन्थावली में इस पाठ को ग्रहण करते हुए भी यह सुझाव दिया है कि कदाचित् मूल-पाठ आहर कहे था और अहरखि उसी का विकृत रूप है। किन्तु आहर शब्द का प्रयोग भी विरल ही है। कुछ स्थल इस सम्बन्ध में विशेष रूप से तुलनीय है, यथा------
(क) आहर सभि करदा फिरै, आहरु इकु न होइ।
नानक जितु आहरि जगु ऊधरै, बिरला बूझै कोइ।।
(- गुरु अर्जुनदेव, गुरुग्रंथ साहब, पृ. 965)
यहाँ इसका अर्थ उद्यम ज्ञात होता है। तुलनीय-वी. एस. आप्टे, संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, आहर- संज्ञा- अकाम्प्लिशिंग, परफ़ार्मिंग (पृ. 91)
(ख) कत तप कीन्ह छांड़ि कै राजू।
आहर गएउ न भा सिधि काजू।।
-जायसीः पदमावत् डा. माताप्रसाद गुप्त-सम्पादित छन्द 204-6)
(ग) जेइं जग जनमि न तोहिं पहिचांनां।
आहर जनम मुएं पछितानां।।
(-मंझनः मधुमालती, मा. प्र. गुप्त-सम्पादित छन्द5-1)
हिन्दी शब्दसागर में पदमावत में प्रयुक्त आहर का उदाहरण देकर इसे सं. अह (दिन) से व्युत्पन्न बताया गया है और इसका अर्थ सयम दिया गया है। किंतु यह व्यत्पत्ति सन्तोषजनक नहीं लगती। डॉ. माताप्रसाद जी ने मधुमालती में इसके विकास का क्रम इस प्रकार दिया हैः सं. अफल >प्रा. अहल>पुरानी हिन्दी आहर (=निष्फल, व्यर्थ)। कबीर, जायसी, और मंझन- इस तीनों के ऊपर उद्धृत- इन तीनों के ऊपर उद्वृत्त प्रयोगों के सम्बन्ध में इस अर्थ की संगति बैठ जाती है। अर्जुनदेव ने चूँकि अफल से व्युत्पन्न आहर का नहीं, प्रत्युत आहर (तत्सम) का ही प्रयोग किया है, अतः उनका अर्थ भिन्न हो गया है। इस प्रकार मन आहर कहं बाउ न कीजै का उपयुक्त अर्थ होगा- ऐ मन, व्यर्थ के लिए विवाद या बकवाद मत कर।
(6) गोंदरी
पद वही पंक्ति 6, काहू गरी गोंदरी नांहीं काहू सेज पयारा। गोंदरी का अर्थ एक टीकाकार ने प्याज़ दिया है, किंतु गोंदरी वस्तुत सं. गुन्द्रा (घास-विशेष ) से बना है जिसका अर्थ है पुवाल या कुश-कास से बनी हुई चटाई। अवधी में अब भी गोंदरा या गोंदरी इसी अर्थ में प्रयुक्त होते है। अतः गरी-गोंदरी नारियल और प्याज़ का बोधक नहीं, बल्कि सडी-गली चटाई का बोधक है।
(7) तनीं-तागरी
पद वही, पंक्ति 10, चिरकुट फारि चुहाड़ा लै गयी तनीं तागरी छूटी। रीति तथा कृष्ण काव्य में तनी और त गड़ी क्रमशः चोलीबन्द और करधनी के अर्थ में बहुत प्रयुक्त हुए है, जैसे- सोहत चोली चारु तनी (-परमानन्ददास, 376) अथवा, अञ्जन नैन तिलक सेंदुर छबि चोली चारू तनी (कुम्भनदास, 317)। भूषन ने चोली के ही अर्थ में इसका प्रयोग किया है, यथाः तनियां न तिलक सुथनियां पगनियां न घामैं घुमरात छोड़ि सेजियां सुखन की। किन्तु कबीर के प्रयोगों से ध्वनित होता है कि उन्होंने इन दोनों वस्तुओं का उल्लेख केवल स्त्रियों के वस्त्राभूषण समझ कर नहीं, प्रत्यत् पुरुषों द्वारा धारण किये जानेवाले उपादान समझ कर किया है ओर इस बात के प्रमाण अन्यत्र भी मिलते है। मिर्ज़ा ख़ाकृत तुहफ़तुल् हिन्द नामक हिन्दी-फ़ारसी कोश में, जिसकी एक हस्तलिखित प्रति इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन, से कुछ समय पूर्व प्रयाग-विश्वविद्यालय के शोधछत्र अचलानन्द जखमोला के निमित्त यहाँ की लाइब्रेरी में आयी थी, पृ. 228 ए पर तनी शब्द के लिए बंदजामा व अम्साले आँ बुवद- टिप्पणी दी हुई है जिससे ज्ञात होता है कि यह बन्दज़ामा की तरह का कोई वस्त्र था जिसे पुरुष भी धारण करते थे। तुलसी ने तनिया को स्पष्ट रूप से कटि भाग का वस्त्र बताया हैः
तनिया ललित कटि, विचित्र टिपारो सीस, मुनि मनहरत वचन कहै तोतरात। तथा कनक रतन मनि जटितरटत कटि किंकिन कलित पांत पट तनियाँ (-- गीतावली, बैजनाथ-सम्पादित, नवकिशोर प्रेस, संस्करण, पृ. 96)
तागड़ी या कटिसूत्र पहले पुरुष भी पहना करते थे। हर्ष में प्राग्ज्योतिषेश्वर के दूत ह्सवेग को मोतियों से बना हुआ परिवेश नामक कटिसूत्र और माणिक्य-खचित तरगण नामक एवं बहुत सी भोजन के सामान भेजा था। (-हर्षचरित एक सांस्कृतिक)
में डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा पृ. 171 पर उद्धृत) शव को जलाते समय उसे समस्त बन्धनों से मुक्त कर देते हैं, अतः अन्तिम समय में तनी-तागड़ी भी उतार लेते है- यही कवि का मूलभाव है। दुर्बोधता के कारण ही विभिन्न प्रतियों में इसके अनेक पाठान्तर मिलते है। उदाहरणार्थ, गुरु-ग्रन्थसाहब में तरी तागरी (प्राचीन नागरी में न और र एक से होते थे। कदाचित् इसी भ्रम से तनी के स्थान पर तरी), दादूपन्थी पोथी में तणी तणगती, निरञ्जनी-सम्प्रदाय की पोथी में तड़ी तामड़ी इत्यादि। प्रस्तुत प्रसंग में कबीर द्वारा प्रयुक्त तनीं तुलसी के तनिया के अधिक निकट का प्रतीत होता है। अतः तनीं तागरी का अर्थ यहाँ कछनी और कटिसूत्र अधिक उपयुक्त जँचता है।
(8) कबिता
पद 75-5, कबित पढ़े पढ़ि कबिता मूए कापड़ी केदारै जाई। यहाँ कबिता काव्य करने वाला अर्थात् कवि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जो आजकल के पाठकों को कुछ विलक्षण-सा लगेगा, किन्तु कुछ मध्यकालीन कवियों में (विशेषतया सन्तों और सूफियों में) इसका समान अर्थ में प्रयोग मिल जाता हैं, जैसे उसमान-कृत चित्रावली के छंद 617 में कवितन्ह चरन कथा कै गाई।
(9) गौंहनि
पद 109-1, मैं सासुरे पिय गौंहनि आई। गौंहनि अर्थात् पास, निकट, साथ। तुल. देवज् गोहन लागे फिरै गहि के गहिरे रंग में गहिराऊ तथा जायसी, भए बरात गोहन सब राजा (----पद्मावत 277-2)। आजकल के शिक्षिता साहित्यिक को, जिसका सम्बन्ध ग्राम्य-जीवन से कम है, यह शब्द अपरिचित सा लगेगा, किन्तु अवधी तथा भोजपुरी में यह शब्द अब भी प्रचलित है। गाँव से सँटी हुई धरती को गौहान या गोहानी कहा जाता है। डॉ. बासुदेव शरण अग्रवाल ने गौहानस गोहना, गोहन आदि को सं. गोबान से व्युत्पन्न माने जाने का प्रस्ताव किया है। (-ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली, भूमिका पृ. 9)। अवधी में गोहन लगुवा उसे कहते है जो छाया की तरह किसी के पीछे लगा रहे।
(10) माहा
पद 111-1, रामुराय चली बिनावन माही। घर छोड़े जाइ जुलाहो। यहां माहो का अर्थ प्रायः सभी टीकाकारों ने माया दिया है, केवल एक राजस्थानी टीकाकार ने इसका अर्थ उत्तम वस्त्र दिया है, जो पर्याप्त सन्तोषप्रद लगता है। ऊँवा कपड़ा माहा सो ऊँची भगति (-दे., कबीरवाणी की एक प्राचीनतम टीका, हिन्दी अनुशीलन, वर्ष 13, अंक 4, अक्टूबर-दिसम्बर 1960)। किन्तु यह शब्द न तो किसी अन्य कवि की रचना में मिल सका है और न किसी कोश में ही।
(11) मिनिऐ
पद वही, - 5, गजै न मिनिऐ तोलि न तुलिऐ। पहजन सेर अढ़ाई। गजै न मिनिऐ पाठ गुरु ग्रन्थसाहब का है जिसके अनेक सरलतर पाठान्तर मिलते हैं जैसे- निरञ्जनी सम्प्रदाय की पोथी में और रज्जब द्वारा संकलित सर्वगी में गजह न मायी बीजक में गज न असाई आदि। किन्तु पाठालोचन के सिद्धान्तों के अनुसार यहाँ अपेक्षाकृत अधिक गूढ़ और कम प्रचलित पाठ मिनिऐ ही ग्रहण किया गया। किन्तु इस शब्द की ठीक पहचान तब तक न हो सकी जब तक कि बखना की निम्नलिखित पंक्तियाँ न मिल गयीः-
गगनि धरणि जिन थाप्या। सो मिण्यां न जाई माप्या।।
(- बखना जी की वाणी, मंगलदास सम्पादित, पद 43-6)
तथा- रतन मिल्यौ पंणि परिख न आई।
तोल्यो जोख्यो मिण्यो न जाई।। (-वही, पद 105-3)
तुल. पाइअ. मिण-स. क्रि. परिमाण करना, मापना। यह शब्द वस्तुतः असीरी बेबिलोनी मिना या मिनह से व्युत्पन्न है जो तौल की एक माप का सूचक है और आर्यों ने असीरी-बेबिलोनी से यह शब्द वेदों में मना के रूप में ग्रहण किया (-सुनीतिकुमार चटर्जी, भारतीय आर्यभाषा और लिपि, पृष्ठ 31)। आगे चलकर मन के रूप में यह अनेक पूर्वी देशों में तौल की एक इकाई बन गया (ई. नॉरिसः ऑन असीरियन ऐण्ड बैबिलोनियन वेट्स-जे. आर. ऐ. एस. ऑव ग्रेटब्रिटेन, खण्ड 16, पृष्ठ 215। किन्तु मध्यकालीन हिन्दी कवियों ने तथा प्राकृत-अपभ्रंश के कवियों ने इसका प्रयोग मापने के अर्थ में (तौलने के अर्थ में नहीं) किया है। अरबी में एक शब्द मिनवाल मिलता है जिसका अर्थ है करघे का वह बेलन जिस पर कपड़ा लपेटा जाता है। कदाचित् इसी आधार पर डॉ. रामकुमार जी ने इसका अर्थ बेलन पर लिपटना किया है (सन्त कबीर, परि., पृ. 16 तथा 144), किन्तु प्रसंग आदि की दृष्टि से और बखना के समान प्रयोग की दृष्टि से इसका ऊपर सुझाया हुआ अर्थ अधिक उपर्युक्त लगता है। इस शब्द के उपयुक्त अर्थ से अवगत न होने के कारण लिपिकारों ने भी उसके अनेक सरलतर पाठान्तर आविष्कृत कर लिये।
(12-13) धौल तथा गड़री
पद 114.3, धौल मंदलिया बैल खाली कउवा ताल बजावै। तथा पंक्ति 7, कहे कबीर सुनहु रे संती गड़री परबत खावा।। कबीर-वाणी की प्राचीनतम उपलब्ध टीका में (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है) धौल का अर्थ उज्ज्वल किया गया है- धौल ऊजल मन सोई मदलिया उसकी आधुनिकतम प्रकाशित टीका में कबीर ग्रन्थावली (ना. प्र. स.) का धौल मदलिया बैलर बाबी पाठ प्रामाणिक मान कर इस पंक्ति का अर्थ किया गया है- ढोल, मृदंग बॉबी आदि विविध वाद्य संसार में माया-आकर्षणों के रूप में बज रहे है, विषय-वासना की और एकदम लपकने वाला कौवा-रूपी जीव भी इन आकर्षणों की गति में अपने को छोड़ देता है। (- प्रो. पुष्पपाल सिंह कबीर-ग्रन्थावली सटीक षष्ठ 296) डॉ. रामकुमार जी न बहुत पहले ही कबीर ग्रन्थावली (ना. प्र. स.) का इस पाठ-विकृति का निर्देश कर दिया था। (सन्त कबीर, प्रस्तावना, पृ. 7)। फिर भी पुष्पपाल सिंह जी को व्यर्थ की ऊहापोह करनी पड़ी। बाँबी कौन बाजा होता है और धौल ढोल का वाचक कैसे हो गया, इसकी ओर उन्होंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। कबीर का धौल हमारी समझ से जायसी के धौर से अभिन्न हैः धौरी पण्डुक कहु पिट ठांऊं। जी चितरोख न दोसर नांऊं। (--पद्मावत 358-4, मा. प्र. गुप्त-सम्पादित)। धौरी को डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने घवर पक्षी बताया है जो फ़ाख्ता की जाति का होता है। इसी प्रकार गड़री की पहचान भी जायसी और उसमान द्वारा प्रयुक्त गुड़रू (एक चिड़िया) से की जा सकती है। तुल. पदमावत 541-4 पर डॉ. अग्रवाल की सञ्जीवनी-टीका और चित्रावली 62-6, उसर बगेरा गुड़रू जावा। गड़री या गुड़रू अवश्य ही कोई छोटी चिडिया होगी जिसके विरोध में पर्वत की विशालता के उल्लेख से कबीर की उल्टबांसी फबती है। किन्तु भ्रमवश कुछ टीकाकारों ने इसे गाडर (=भेड) का पर्याय समझ लिया। पुष्पपाल सिंह जी ने तो इसे गड़रिन (=भेंड़ चरानेवाली) तक मान लिया। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि भेंड़ के लिए कबीर ने गाड़र शब्द का ही प्रयोग किया है। जैसे गाड़र आंनीं ऊन कीं बांधी चरैं कपास। यदि यहाँ भी गाड़र (=भेड) ही उनका अभीष्ट होता तो समान मात्रा का शब्द होने के कारण उसे भी सरलता से रखा जा सकता था, फिर भी कबीर ने गड़री का प्रयोग किया जिसका तात्पर्य यह है कि अवश्य ही गाड़र से भिन्न अर्थ का धोतक है।
(14) पढ़िया
पद 119-1, जाइ पूछौ गोविन्द पढ़िया पण्डिता तेरा कौन गुरू कौन नेला। विशेष बात यह है कि पढ़िया यहाँ क्रियापद के रूप में नहीं, बल्कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। (सं. पढिया>प्रा. पढिया अया. और पुरानी हिन्दी पढ़िया)। ठीक इसी स्वर में गोरखनाथ ने भी पढ़िया का प्रयोग पण्डित के लिए किया है, तुल. गोरखबानी सबदी 22-2, ससंबेद गुरु गोरख कहिया बूझिले पण्डित पढिया तथा पद 18-9 यह परमारथ कहौ ही पण्डित रुग जुग स्यांम अघरबन पढ़िया।
इस प्रकार हम देखते है कि कबीर ने तत्कालीन जन-समाज में प्रचलित ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया है जिनका ठीक-ठाक अर्थ समझने के लिए हमें अन्य मध्यकालीन कवियों तथा प्राकृत एवं अपभ्रंश के कवियों विशेषतया नाथ योगियों तथा बौद्ध सिद्धों की रचनाओं का भी अनुशीलन करना पड़ता है, साथ ही अवधी, भोजपुरी आदि जनपदीय बोलियों की ठेठ शब्दावली से भी परिचय प्राप्त करना अपेक्षित हो जाता है अन्यथा ऐसे स्थलों पर हमें भ्रम हो जाना स्वाभाविक है।
सन्दर्भ संकेत
1. अपने वरिष्ठ सहयोगी डॉ. जगदीश गुप्त के सुझाव पर मैंने थिलगबेश (बेबिलोनी-मसारी आख्यानों में वर्णित एक अपरिमेय शक्ति के योद्धा) सम्बन्धी साहित्य का अवलोकन कर उससे इस शब्द के सम्बन्ध की सम्भावनाओं पर विचार किया। गिलगमेश अपने परवर्ती हरकुलीस की भाँति अत्यन्त शक्तिशाली था और उरुक नामक महान् नगर का अधिपति था। प्राचीनतर अभिलेखों में इसका नाम इज़दुबार मिलता है। हौष्ट नामक जर्मन विद्वान् ने गिलगमेश सम्बन्धी प्राचीन आख्यान का संग्रह कर उसका सम्पादन किया है। उसने इबनी (आधा नर और आधा पशु), अलु (अत्यन्त भयंकर साँड़) और खम्बावा को पराजित किया था और सिंह से भी लड़ाई की थी। अनेक प्राचीन मुद्राओं में गिलगमेश को भयंकर साँड़ तथा सिंह से लड़ते हुए चित्रित किया गया है। (जास्ट्रोः रेलिजन ऑव बैबिलोनिया ऐण्ड असीरिया, पृष्ठ 488)। भारतीय पौराणिक देवताओं में से अनेक बैबिलोनी देवताओं से मिलते है। तुलनार्थ, बालि-बेबि. बेल (पाताल का देवता), पार्वती- बेबि. निन खर-सग (महान् पर्वतों की देवी), सरस्वती-बेबि. बाउ (सं. वाक)। गिलगमेश यद्यपि नृसिंह-रूप तो नहीं, किंतु देवत्व और मनुजत्व का सम्मिश्रण माना गया है। और फिर दोनों शब्दों में ध्वनि-साम्य भी है। अतः दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध की कल्पना निराधार नहीं कहीं जा सकती। फिर गिलारना क्रिया का अर्थ नृसिंहवत् या सिंहवत् गरजना किया जाएगा। फिर भी इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में अभी निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.
