जायसी और प्रेमतत्व पंडित परशुराम चतुर्वेदी, एम. ए., एल्.-एल्. बी.
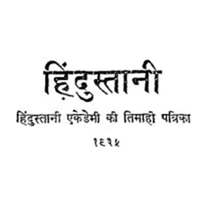
जायसी और प्रेमतत्व पंडित परशुराम चतुर्वेदी, एम. ए., एल्.-एल्. बी.
हिंदुस्तानी पत्रिका
MORE BYहिंदुस्तानी पत्रिका
रोचक तथ्य
Jayasi or Premtataw, Anka-3, 1934
जायसी की रचना पद्मावत की प्रेम-गाथा द्वारा अथवा उन के ग्रंथ अखरावट में वर्णन किए गए सिद्धांतों द्वारा जिस प्रेमतत्व का परिचय मिलता है वह वास्तव में बहुत ही उच्च व गंभीर है और उस के महत्व का पता हमे पहले-पहल उस समय चलता है जब कि, हीरामन तोता द्वारा पद्मावती के रूप व गुण का संक्षिप्तमात्र समाचार पाते ही, राजा रतनसेन उस के प्रेम में पड़ कर कह उठता है-
तौनि लोक चौदह खंड, सबै परै मोहिं सूझि।
प्रेम छाँडि नहिं लोन किछु, जो देखा मुन बूझि।।
अर्थात् अब मुझे तीनों लोक और चौदहों भुवन प्रत्यक्ष हो गए और मैं ने अपने मन में समझ बूझ कर देख लिया कि वास्तव में प्रेम के समान कोई भी वस्तु सुंदर नहीं हो सकती। अभिप्राय यह है कि संसार की किसी भी वस्तु में ऐसी सुंदरता नहीं मिल सकती जो प्रत्येक स्थिति अथवा दशा में भी एक समान हो कर वर्तमान रहे। यह प्रेम की ही विशेषता है कि,
मुहमद बाजी प्रेम कै, ज्यों भावै त्यों खेल।
तिल फूलहिं के संग ज्यों, होइ फुलायल तेल।।
अर्थात् प्रेम की बाज़ी किसी प्रकार भी खेली जाय उस में लाभ ही लाभ है जैसे तिल के दाने, फूलों के सहवास के उपलक्ष में यदि पेरे भी जाते है तो अंत में उन का रूप सुंगधित लेत बन कर ही प्रकट होता है। प्रेम के कारण अथवा प्रेम का परिणाम-स्वरूप दुख हो ही नही सकता। इस का तो नियम ही है कि-
प्रेम कै आगि जदै जौं कोई।
दुख तेहि कर न अँविरथा होई।।
अर्थात् प्रेम की ज्वाला में अपने को भस्मात् कर देने वाले का दुःख कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस के दुःखों के साथ ही साथ सुख भी लगा ही रहता है जिस कारण उस के आनंद में बाधा नहीं पड़ पाती और-
दुख भीतर जो प्रेम-मधु राखा।
जग नहिं मरन सहै जो चाखा।।
अर्थात् प्रेम की पीर के साथ ही जो माधुर्य अनुभव में आता है उस का स्वाद इतना तीव्र होता है कि उस के सामने संसार में मरण तक का कष्ट हँसते-खेलने सह लेना कोई असंभव बात नहीं। इस कारण प्रेम नितांत रूप से सदा एख-सम समझा जाता है और इस की एकरसता ही इस के वास्तविक सौंदर्य का कारण है। इस अनुपम गुण के ही संयोग से-
मानुष प्रेम भएउ बैकुंडी।
नाहिंत काह छार भर मूठी।।
अर्थात् इस प्रेम के ही कारण मनुष्य अमरत्व तक प्राप्त कर लेता है, नहीं तो इस मूठी भर छार मात्र से बने हुए मिट्टी के पुतले से हो ही क्या सकता था? अतएव कवि को इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि-
प्रेम पंथ जौं पहुँचे पारा।
बहुरि न मिलै आइ एहि छारा।।
अर्थात् जो मनुष्य प्रेममार्ग का पथिक होकर पार पहुच गया वह फिर मिट्टी से ही मिलते के लिए इस क्षणभंगुर शरीर को धारण कर नहीं सकता। वह अमर हो जाता है।
परंतु प्रेम जितना ही सुदंर औऱ मनोहर है उतना ही उस का मार्ग भी विकट और दुर्गम है क्योंकि इस पर चलने वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने साधन की सरलता अथवा कठइनता को अपने विचार से एक दम निकाल दे और ऐसा करने के कारण प्रायः देखा गया है कि उस के मार्ग का ढंग ही विचित्र हो जाता है। वह जितना ही उलटे रास्ते से चले और जितना ही कष्ट झेले उतना ही अपने को, उद्देश्य की पूर्ति करता हुआ, पाता है। इसी लिए कवि का कहना भी है कि-
उलटा पंथ प्रेम के वारा।
चढै सरग जो परे पतारा।।
अर्थात् प्रेम का मार्ग ही विपरीत है क्योंकि इस के द्वारा स्वर्ग पर जाने के अधिकारी वही बन सकते है जिन्होंने पहले अपने को पाताल में डाल दिया हो। इस का अनुसरण करने के प्रथम ही यह समझ लेना आवश्यक है कि अब हमे अपने दुख-सुख की कोई परवा नहीं करना है। सिहल-द्वीप जाते समय मार्ग में पड़ने वाले विस्तृत समुद्र को पार करने की कठिनाइयों का ब्यौरा, केवट द्वारा, सुन कर, प्रेमी राजा रतनसेन इसीलिए सहसा कह उठता है कि-
राजै कहा कीन्ह मैं प्रेमा।
जहाँ प्रेम करूँ कूसल खेमा।।
अर्थात् जब मैने प्रेम का मार्ग ग्रहण कर लिया तो अब कुशल क्षेम के लिए किसी प्रकार की आशा करना ही व्यर्थ है क्योंकि नियमानुसार प्रेम के रहते कुशल क्षेम का होना असंभव सी बात है। प्रेम करनेवाले को दुख झेलना ही पड़ेगा। कवि ने इश बात को स्पष्ट करते हुए कई स्थलों पर बहुत से उदाहरण भी दिए है। जैसे-
प्रेम-फाँद जो परा न छूटा।
जीउ दीन्ह पै फाँद न टूटा।।
गिरगिट छंद धरै दुख तेता।
खन खन पीत रात खन सेता।।
जान पुछार जो या बनवासी।
रोंव रोंव परे फँद नगवासी।।
पाँखन्ह फिरि फिरि परा सो फाँदू।
उड़ि न सकै अरुझा भा बाँदू।।
मुयों मुयों अहनिसि चिल्लाई।
ओही रोस नागन्ह धै खाई।।
पंडुक, सुआ, कक वह चीन्हा।
जेहिं गिउ परा चाहि जिउ दीन्हा।।
तीतिर-गिउ जो फाँद है, नित्ति पुकारै दोख।
सो कित हँकारि फाँद गिउ (मेलै) कित मारे होइ मोख।।
जानहिं भौर जो तेहि पथ लूटे।
जीउ दीन्ह औ दिपहु न छूटे।
अथवा,
ओहि पथ जाइ जो होइ उदासी।
जोगी, जती, तपा सन्यासी।।
भोग किए जौं पावत भोगू।
तजि सो भोग कोई करत न जोगू।।
साधन्ह सिद्धि न पाइये, जौ लगि सधै न तप्प।
सोपै जाने बापुरा, करै जो सीस कलप्प।।
का भा जोग-कथनि के कथे।
निकसै घिउ न बिना दुधि मथे।
जौ लहि आप हेराइ न कोई।
तौ लहि हेरत पाव न सोई।।
प्रेम पहार कठिन विधि गढ़ा।
सो पै चढै जो सिर सौ चढा।
पंथ सूरि कर उठा अँकूरू।
चोर चढ़ै की चढ़ मंसूरू।।
और,
ना जेइ भएउ भौर कर रंगू।
ना जेइ दीपक भएउ पतंगू।।
ना जेइ करा भृंग कै होई।
ना जेई आपु मरै जिउ खोई।।
ना जेई प्रेम औटि एक भएऊ।
ना जेहि हिये माँझ डर गएऊ।।
तेहि का कहिय रहव जिउ, रहै जो पीतम लागि।
जौं वह सुनै लेइ धँसि, का पानी का आगि।।
अर्थात् प्रेम के फंदे में जो पड़ गया वह कभी नहीं छूटता। प्राण दे देने पर भी उस के फंदे का टूट जाना कठिन है। गिरगिट को अनेक कष्ट झेल कर भी क्षण-क्षण पर पीले, लाल अथवा श्वेत रंग का होना पड़ता है। मोर को वन में रहकर अपना रोम-रोम नागपाश में डालना पड़ता है, जिस के कारण उस के पंख पर फंदे के चिन्ह तक पड़ जाते है और वह बंदी हो कर उड़ने में असमर्थ हो जाता है, वह रात-दिन मुयों, मुयों कहकर चिल्लाया करता है और क्रोध में आकर दौड़-दौड़ कर साँपों को खाता फिरता है। इस फंदे का चिन्ह, इसी प्रकार, पंडुक तोते और नीलकंठ पक्षियों के भी गले में पड़ा दीखता है जिस के कारण उन्हें प्राण तक निछावर करने पड़ते हैं और तीतर के गले पर दीखने वाला चिन्ह इतना अशुभ-सूचक है कि या तो उस के द्वारा इसे बंधन स्वीकार करना पड़ता है अथवा मुक्त होने पर भी लड़कर मरना पड़ता है अर्थात् इसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। फिर भ्रमर तो इस मार्ग का पथिक हो कर एक दम लुट ही जाता है, उसे प्राणों की आहुति देने पर भी छुटकारा नहीं मिलता। इसी लिए इस मार्ग का अनुसरण भरसक उसी को करना चाहिए जो उदासी, योगी, यती, तपस्वी अथवा संन्यासी हो, क्योंकि भोग-विलास में पड़े हुए को ही यदि यहाँ सफलता मिल सकती तो ये लोग भोगों का त्याग कर कठिन व्रत की साधना करने पर आरूढ़ नहीं होते। प्रेम-प्राप्ति की सिद्धि केवल साध करने मात्र से नहीं हो सकती इस के साथ-साथ तप की साधना भी आवश्यक है। इसे वही अनुभव कर पाता है जो अपने शीश को पहले धड़ से अलग कर डालता है। केवल कथनी कथने से कुछ नहीं होता। घी के निकालने के लिए दही को पहले भली-भाँति मथने की आवश्यकता पड़ती है। जब तक अपने आप को भी, ढूँढते-ढूँढते कोई न खो दे तब तक उसे पा ही नहीं सकता। प्रेम के पहाड़ की रचना ही कुछ ऐसी अनोखी है कि उस पर चढ़ने वाले को पैरों द्वारा न चलकर सिर के बल जाना पड़ता है। यह वास्तव में, सूली का मार्ग है जिस पर या तो चोर चढ़ाया जाता है अथवा मंसूर ऐसे मनुष्य का बलिदान होता है। बात यह है कि जिस के भ्रमर का रंग धारण नहीं किया, जो दीपक देख कर पतंग नहीं बन गया, जिस पर भृंग का प्रभाव नहीं पड़ा अथवा जिस ने अपने प्राणों का उत्सर्ग नहीं कर दिया और न जो प्रेम के कारण तपाया जा कर एक हो गया अथवा जिस के हृदय से भय का लोप न हुआ उसे प्रियतम के प्रति सच्चा अनुराग हो ही नहीं सकता और न वह उस के लिए आग या पानी में पड़ सकता है।
प्रेमी की अवस्था ही विचित्र हो जाती है। प्रेम के प्रभाव द्वारा अभिभूत होकर उस की मनोवृत्ति इस प्रकार बदल जाती है कि उसे हित-अनहित की बातों की पहचान तक नहीं रह जाती और वह-
उपजी प्रेम पीर जेहि आई,
परबोधत होइ अधिक सो आई।
अमृत बात कहत विष जाना,
प्रेमक वचन मीठ कै माना।
अर्थात् जिस के हृदय में प्रेम की कसक बैठ गई उसे यदि समझाया बुझाया जाय तो उस पर प्रभाव उलटा ही पड़ा करता है और पीड़ा कम होने की जगह बढ़ने लगती है। प्रेम के आवेश में उसे भली से भली बात बुरी जान पड़ती है और वह केवल प्रेमसंबंधी वार्तालाप को ही अपने अनुकूल समझा करता है। वह अपने शरीर तक की रक्षा के विचार से इस प्रकार उदासीन हो जाता है कि उसे किसी बात की परवा ही नहीं रहती। क्योंकि-
जेहि के हिये प्रेम-रंग जामा।
का तेहि भूख नींद बिसरामा।।
अर्थात् जिस के हृदय में प्रेम ने रंग जमा लिया उस के लिए भूख, निंद्रा अथवा विश्राम का आना असंभव है। उसे शांति मिल ही नहीं सकती। उस की मानसिक स्थिति का वर्णन करता हुआ स्वयं राजा रतनसेन पद्मावती से कहता है कि-
सुनु, धनि! प्रेम-सुरा के लिए।
मरन जियन डर रहै न हिए।।
जेहि मद तेहि कहाँ संसारा।
की सो घूमि रह की मतवारा।।
सो पै जान पियै जो कोई।
पी न अघाइ जाइ परि सोई।।
जा कँह होइ बार एक लाहा।
रहै न आहि बिनु आही चाहा।।
अरथ दरव सो देइ बहाई।
की सब जाहु न जाइ पियाई।।
रानिहु दिवस रहै रस-भीजा।
लाभ न देख न देखै छीजा।।
अर्थात् हे प्यारी, प्रेम वास्तव में, मदिरा के समान है जिस का पान करते ही जीवन मरण तक का भय एक मद जाता रहता है, जिस ने एक बार भी इसे पी लिया उस के लिए यह संसार कुछ भी नहीं है और वह मद के कारण मतवाला होकर डोलता फिरता है। इस की मादकता का प्रभाव वही जानता है जो इसे पीता है और पीकर तृप्त होना नहीं जानता ब्कि पीते पीते निद्रा में मग्न हो जाता है। जिसे एक बार भई इस की प्राप्ति हो गई वह इस के बिना रह ही नहीं सकता और सदा इस के लिए अधीर हुआ फिरता है। अपनी सारी संपति को तिलांजलि देकर मानो वह मन में ठान लेता है कि चाहे सब कुछ चला जाय किंतु मैं इस रस का आस्वादन नहीं छोड़ सकता। अतएव रात दिन वह इसी रस में अपने को भिगोये रहा करता है और अपने लाभ अथवा हानि की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता। प्रेमी अपने को, एक प्रकार से एक दम खोकर, अपना अस्तित्व ही नष्ट कर देता है जिसे स्पष्ट करते हुए जायसी ने राजा रतनसेन की अवस्था का चित्र इस प्रकार खींचा है-
बूँद समुद्र जैस होइ मेरा।
गा हेराइ अस मिलै न हेरा।।
रंगहि पान बिला जस होई।
आपहि खोइ रहा होइ सोई।।
अर्थात् जिस प्रकार बूद का समुद्र में मिलन हो जाय औऱ वह ढूंढने पर भी न मिल सके अथवा जिस प्रकार पान का पत्ता रंगों में मिल कर अपना अस्तित्व खो बैठे उसी भाँति राजा ने अपने को खोकर प्रेम में मिला दिया और प्रेमी एवं प्रेमपात्र मानों दो से एक हो गए। प्रेम के प्रभाव का इस से उत्कृष्ठ उदाहरण और क्या हो सकता है?
जायसी के अनुसार, इस प्रकार, प्रेम एक नित्य, सुंदर, एक-रस एवं एकांतिक आनंदप्रदायक पदार्थ है जिस के उपलक्ष में प्रेमी को भाँति-भाँति के कष्ट झेलने पड़ते है और, यदि अवसर आ जाय तो, इस के लिए अपने प्राणों तक ही आहुति देना अनिवार्य हो जाता है। प्रेम की मनोवृत्ति इतनी प्रबल है कि वह सदा एक-भाव बनी रहने के लिए प्रेमी को बाध्य किए रहती है, जिस से उस का सारा जीवन ही एकोन्मुख एवं एकनिष्ठ हो जाता है और वह दूसरे किसी काम का नहीं रह जाता है। वह अपने को अपने प्रेमपात्र के हाथ सदा के लिए बेच-सा देता है, जिस कारण उस के छोटे-बड़े सभी काम इस एक ही निमित्त से किए गए जान पड़ते हैं और वह प्रेम से भिन्न किसी दूसरी बात की ओर जा ही नहीं सकता। वह रात दिन प्रेम के नशे में चूर अथवा प्रेम के आनंद में विभोर हुआ रहता है और उसे अपनी सुध तक नहीं रह जाती। प्रेम का प्याला एक बार होठों लगते ही प्रेमी की मानो कायापलट सा हो जाता है और वह यकायक अपनी वर्तमान अवस्था का परित्याग कर एक विचित्र जगत में प्रवेश करता है, जहाँ की सारी वस्तुएं उस के मानसिक रंग में ही रंजित होने के कारण, अपने अभीष्ट मनोराज्य का स्थापित करना उस के लिए सुलभ प्रतीत होने लगता है और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के साधन में सहसा आत्म-समर्पण कर बैठता है। अतएव उस के सभी कार्य, श्वास-प्रश्वास अथवा जीवन-मरण तक इसी के हेतु निश्चित हो जाते है और इस के प्रभाव द्वारा पूर्णतः अभिभूत होने के कारण वह इस के मार्ग की बाधाओं को एकदम तुच्छ गिनने लगता है।
प्रेम के मनोवृत्ति के अंतर्गत, जायसी के अनुसार, किसी पदार्थ के आत्मसात् करने का अभिलाषा अथवा चाह का होना परमावश्यक है और इस बात को उन्होंने हीरामन तोता द्वारा पद्मावती का रूप-वर्णन कराकर राजा रतनसेन के हृदय में तथा राजा रतनसेन के प्रेम एवं प्रयत्न की कथा कहला कर पद्मावती के मन में एक दूसरे को देखने के लिए तीव्र उत्कंठा की उत्पत्ति द्वारा स्पष्ट किया है। यह दर्शन की लालसा, उसी प्रकार, राघव चेतन द्वारा पद्मावती की प्रशंसा सुनने के उपरांत बादशाह अलाउद्दीन के हृदय में उत्पन्न हुई चाह के समान नहीं है। क्योंकि जिस वस्तु को अपनाने के लिए राजा रतनसेन उत्सुक होता है वह उस के लिए वास्तव में एक अपनी ही चीज़ है जो दुर्भाग्यवश सात समुंदर पार पड़ गई है और जिस की सूचना उस के लिए, एक बार फिर से स्मरण करा देने का ही काम करती है, उस का कोई नवीन परिचय नहीं देती। परंतु अलाउद्दीन की अभीष्ट वस्तु एक दूसरे राजा की अपनी विवाहित पत्नि है, जिस का वर्णन सुनकर वह एक प्रकार की कामवासना की तृप्ति के निमित्त यकायक अधीर हो जाता है। अलाउद्दीन की चाह उस की भोगलिप्सा से रंजित होने के कारण वास्तविक प्रेम के महत्व को नहीं पहुँचती, किंतु राजा रतनसेन की अभिलाषा का आधार, कोई रहस्यपूर्ण पूर्व-संबंध होने के कारण, उस की दर्शनोत्कंठा का रूप आरंभ से ही विरह-रंजित सा दीख पड़ता है, जिस कारण हम राजा रतनसेन के पूर्वनुराग को ही पूर्ण वियोग में परिणत पाते है।
उक्त रहस्यपूर्ण पूर्व-संबंध का परिचय जायसी ने स्पष्ट शब्दों में कही नहीं किया है, जिस कारण, सच्चे एकनिष्ठ प्रेम के लिए पहले किसी एक निर्दिष्ट भावना का होना परमावश्यक मानकर, उस के अभाव में, राजा रतनसेन का केवल रूपवर्णन सुनते ही विरह के वशीभूत हो जाना अनुपयुक्त एवं नक़ली तक समझा गया है। परंतु, वास्तव में, ऐसा समझना ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि पहले तो जायसी ने अपनी प्रेमगाथा की रचना प्रधानतः भारतीय पद्धति के ही अनुसार की है और प्रायः सारी सामग्री तक भारतीय भांडार से ही लिया है, जिस कारण उन के मुस्लिमधर्मावलंबी होते हुए भी इस रचना में हिंदुओं के जन्मांतरवाद की छाया का पड़ना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। दूसरे जिस प्रेमतत्व को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने इस रचना का आरंभ किया था वह मूलतः ईश्वरोन्मुख प्रेम है जो कि सारे ब्रह्मांड के मूलाधार जगन्नियंता परमेश्वर के प्रति उद्दिष्ट होने के कारण धरम के प्रीति बनकर सब के हृदय में एख समान ही आविर्भूत हो सकता है और जिस में, सूफी-संप्रदायवालों के सिद्धांतानुसार, परमात्मा से बिछुड़ी हुई जीवात्मा की विरहव्यथा का आरंभ से ही वर्तमान रहना अनिवार्य-सा है। जायसी ने इन दोनों कारणों के संकेत अपने ग्रंथ पद्मावत में दिए है किंतु, उन के उद्देश्यनुसार, प्रधानता दूसरे को ही मिली है। अतएव प्रेमतत्वविषयक जायसी की विशिष्ट भावना को ध्यान में रखते हुए उन के कथा-वर्णन के किसी अंश को सहसा अस्वाभाविक बतला देना भ्रम-रहित नहीं कहा जा सकता।
उक्त पूर्व-संबंध की ओर संकेत करते समय जायसी ने राजा रतनसेन के निमित्त पद्मावती का पूर्वानिश्चित संबंध, इन दोनों बातों, के विषय में उल्लेख किया है। राजा रतनसेन के बचपन में ही उस की सामुद्रिक रेखाओं को देखकर पंडित कह देता है कि-
रतनसेन यह कुल निरमरा।
रतनजोति मनि माथे परा।।
पदुम पदारथ लिखी सो जोरी।
चाँद सुरुज जस होइ अँजोरी।।
अर्थात् यह रतनसेन अपने कुल को उच्च बनानेवाला है, इस के मस्तक पर एक विशेष ज्योतिस्वरूप चिन्ह दिखलाई देता है। इस कारण इस की जोड़ी के लिए पद्मपदार्थ (पद्मावती) निश्चित है और इन दोनों का संयोग सूर्य-चंद्रमा के संयोग के समान उजियाला कर देगा। इसी प्रकार पद्मावती का सपन विचारू बतलाती हुई उस की सखी कहती है कि-
पच्छिउं खंड कर राजा कोई।
सो आवा वर तुम्ह कहं होई।।
चाँद सुरुज सौं होइ बियाहू।
वारि विधंसव वेधब राहू।।
जस ऊषा कहं अनिरूध मिला।
मेटि न जाइ लिखा पुरबिला।।
अर्थात् तुम्हारे स्वप्न का हाल जानकर यह प्रतीत होता है कि पश्चिम देश का कोई राजा आया है, वही तुम्हारा वर होनेवाला है। तभी सूर्य और चंद्रमा का मिलन होगा और सारी विघ्न बाधाएँ नष्ट हो जायँगी। यह संयोग भी उसी प्रकार पूर्वलिखित और अवश्यंभावी है जिस प्रकार प्रसिद्ध ऊँचा और अनिरुध का समागम था। यह किसी भी प्रकार मिटाएं मिट नहीं सकता। इन बातों से स्पष्ट जान पड़ता है कि कवि, यहां पर राजा रतनसेन एवं पद्मावती के पारस्परिक प्रेम का कारण उन के पूर्व-विधानविहित नियमों अथवा पूर्व-संस्कारों के ही अंतर्गत निर्दिष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है।
इसी प्रकार, प्रेमद्वार अभिभूत राजा रतनसेन के हृदय में ढाढ़स उत्पन्न कर के, उसे विचलित होने से बचाने के लिए, जो बातें सिंहलद्वीप के देव-मंडप में सबद अकूत अथवा आकाशवाणी द्वारा, कहलाई गई हैं उन से भी पता चलता है कि कवि के विरहसंबंधी क्या विचार है तथा प्रेम और विरह के वास्तविक रहस्य का उद्धाटन वह किस प्रकार करता है। जैसे-
प्रेमहिं माँह विरह रसरसा।
मैन के घर मधु अमृत वसा।।
अर्थात् जिस प्रकार मोम के घर अथवा मधुकोश में अमृतरूपी मधु संचित रहा करता है उसी प्रकार प्रेम के अंतर्गत विलह भी निवास करता है। विरह को सदा सच्चे प्रेम के भीतर निहित समझना चाहिए, क्योंकि, कवि के अनुसार, वास्तव में विरह ही वह मूल पदार्थ है जिस में अमरत्व का गुण वर्तमान है और जिस के लिए प्रेम का आविर्भाव हुआ करता है। दूसरे शब्दों में प्रेम का अस्तित्व यदि है तो, वह विरह के ही कारण है क्योंकि वही प्रेम का सार है। अतएव, धरम क प्रीति अर्थात् सच्चे प्रेम की उत्पत्ति के साथ ही विरह का भी जाग्रत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं और न, इसी लिए, “रूप वर्णन सुनते ही रतनसेन के प्रेम का जो प्रबल और अद्म्य स्वरूप दिखाया गया है” वह अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है। कवि का उद्देश्य पद्मावत में राजा रतनसेन अथवा पद्मावती को, वस्तुतः साहित्यिक नायक अथवा नायिका के रूप में चित्रित करने का नहीं था इस लिए पूर्वानुराग में भी पूर्ण विरह के लक्षणों का अनुभव कर दोषारोपण करना ठीक नहीं।
जायसी ने अपने निर्दिष्ट प्रेममार्ग को इस विरह के ही कारण अत्यंत विकट एवं दुर्गम भी बतलाया है क्योंकि विरह, इन के अनुसार, संसार की सभी कठोर वस्तुओं से भी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण है। विरह को वे एक प्रकार की प्रचंड ज्वाला के समान बतलाते हैं और कहते है कि-
जग महँ कठिन खड़ग कै धारा।
तेहि तें अधिक विरह कै झारा।।
अर्थात् संसार में सब से कठिन वस्तु तलवार की धार हुआ करती है किंतु विरह की ज्वाला उस से भी कहीं अधिक प्रबल और कष्टदायक सिद्ध होती है। इन दोनों में कोई समानता ही नहीं।
बिरहा कठिन काल कै कला।
बिरह न सहै काल बरु भला।।
फाल काढ़ि जिउ लेइ सिधारा।
विरह-काल मार पर मारा।।
विरह आगि पर मेलै आगी।।
विरह घाव पर घाव बजागी।।
विरह बान पर बान पसारा।
विरह रोग पर रोग सँचारा।।
विरह साल पर साल नवेला।
विरह काल पर काल दुहेला।।
अर्थात् विरह क्रूर काल का ही रूप है तब भी काल का आक्रमण सहा जा सकता है, परंतु विरह नहीं सहा जाता। इस का कारण यह है कि काल तो केवल प्राणों को ही लेकर चला जाता है, किंतु विरह मरे हुए को भी मारने पर उद्यत रहा करता है। यह आग पर अधिक आग डाल देता है, घावों पर घाव पैदा करता है, बाण पर बाणों की बौछार किया करता है, रोग पर नए रोग बढ़ाता है, कसक के अंदर कसक चुभाता रहता है, जिस कारण इस का प्रभाव काल के भी ऊपर काल के आक्रमण के समान है। विरह के बराबर, मनुष्य के लिए, कोई वस्तु असह्य नहीं।
परंतु, जायसी के अनुसार, उपरोक्त विरहतत्व की व्यापकता केवल मानवजाति तक ही सीमित नहीं समझी जा सकती। यह विरह ब्रह्माण्ड के अन्य अंशों तक भी अपना प्रभाव डाले नहीं रहता। यह एक वज्राग्नि है और-
विरह के आगि सूर जरि काँपा।
रातिहि दिवस जरै ओहि तापा।।
खिनहि सरग खिन जाइ पतारा।
थिर न रहै एहि आगि अपारा।।
अर्थात् विरहाग्नि की ज्वाला के ही प्रभाव में आकर स्वयं सूर्य तक रात दिन जलता और काँपता रहता है। एक क्षण के लिए भी वह स्थिर नहीं रहता बल्कि कभी स्वर्ग और कभी पाताल की ओर उस का आना-जाना लगा रहा करता है। जायसी ने कहीं कहीं प्राकृतिक वस्तुओं को विरही रतनसेन के व्यथित हृदय, नागमती के अश्रुबिंदु अथवा विरहपत्रादि के द्वारा भी प्रभावित होना दिखलाया है, जिस कारण किसी किसी ने केवल इतना ही समझा है कि उन का अभिप्राय इस “हृदयहारिणी और व्यापकत्व-विधायिनी पद्धति” द्वारा “बाह्य प्रकृति को मूल आभ्यंतर जगत् का प्रतिबिंब सा” दिखाना मात्र था। किंतु ऐसा समझना उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि उपरोक्त अवतरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कवि को ब्रह्मांड की वस्तुएं, वास्तव में, अपने मूल-कारण परमात्मा से बिछुड़ी हुई होने के कारण, स्वयं भी विरह-व्यथित सी समझ पड़ रही है। जायसी की इस समझ का स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित पंक्तियों से भी किया जा सकता है। जैसे-
बिछुरे ससि रवि, मन! नयननि तें पावत दुख बहुतेरो।
भ्रमत स्रमित निसि दिवस गगन महँ तहँ रिपुराहु बड़ेरो।।
जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिहुँ पुर सुजस घनेरो।
तजे चरन अजहूँ न मिटत नित बहिवो ताहू केरो।।
अर्थात् ऐ मन! स्वयं चंद्रमा एवं सूर्य तक उन (विराट्-स्वरूप परमात्मा की) आँखों से विमुक्त होने के कारण ही अनेक दुःख झेलते रहते है, वे आकाश में घूम-घूम कर रात दिन थकते रहते है और अपने प्रबल शत्रु राहु का भय भी उन्हें सदा बना रहता है। इसी प्रकार यद्यपि गंगा नदीं अत्यंत पवित्र है और उस का यश भी चारों ओर फैला हुआ है, किंतु उक्त भगवान् के चरणों से अलग हो जाने के ही कारण उस का भी व्यग्र होकर निरंतर बहते रहना आज तक नहीं छूट पाया है।
अतएव जायसी-द्वारा निद्रिष्ट प्रेमतत्व का विशेषता उस के मूलत विरहगर्भित होने में ही प्रत्यक्ष होती है और उक्त विरह के महत्व को लक्ष्य कर के ही उन्होंने प्रेम के मार्ग को इतना कठिन और दुस्तर बतलाया है। इस प्रेम का आधार स्वयं परमात्मा एवं सारे ब्रह्माण्ड की एकता में सन्निहित है जिस को भूल जाने के कारण सारी सृष्टि आरंभ से ही पूर्ण बिरही की भाँति निरंतर बेचैन बनी डोलती चली आ रही है। मूल-संबंध पर आश्रित रहने के कारण प्रेम इतना उच्च, आकर्षक और चिरस्थायी है और विरह का आदि-स्रोत आदिसृष्टि के मूलविच्छेद में ही वर्तमान रहने के कारण वह इतना व्यापक, महत्वपूर्ण अथवा अनिवार्य सिद्ध होता है। अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगते ही मनुष्य को पुरानी बाते स्मरण में आ जाती हैं और वह सोचता है-
हुता जो एकहि संग, हौ तुम काहे बीछुरा?
अब जिउ उठै तरंग, मुहमद कहा न जाइ किछु।।
अर्थात् सदा एक ही साथ रहने वालों में किस प्रकार वियोग हो गया जिस से आज हृदय में भाँति-भाँति के भाव पैदा हो रहे हैं और अपनी विचित्र स्थिति का हाल कहते नहीं बनता! जायसी ने जीवात्मा एवं परमात्मा के आरंभिक विच्छेद अथवा जीवात्मा द्वारा परमात्मा की मूलविस्मृति का कारण किसी काल्पनिक नारद को बतलाया है, जो देखने में इस्लामी मज़हब के ग्रंथों में वर्णित शैतान के समान जान पड़ता है, किंतु उस के विघ्नोत्पादक ढंगों पर विचार करते हुए, हम उसे हिंदू योगशास्त्रादि ग्रंथों में बतलाए गए, साधकों के मार्ग में आने वाले, विविध अंतरायों का समष्टिरूप ही कह सकते है।
जायसी-द्वारा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार, इसी कारण, प्रेम मार्ग को वास्तविक सफलता का रहस्य आत्मदर्शन अथवा अपने आप की पहचान के भीतर छिपा हुआ है, जिस के लिए प्रेमी को अपने अंतर्जगत के साधने की आवश्यकता हुआ करती है। अतएव जायसी के प्रेमतत्व में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है, तथा इसी कारण, कथावस्तु का निर्वाह करते समय भी कवि ने नायक के लोककर्तव्य से अधिक उस के ऐकांतिक शुद्ध आदर्श की ही ओर ध्यान देना उचित समझा है। जायसी का पद्मावत एक प्रकार का द्वयर्थक काव्य है जिस में राजा रतनसेन और पद्मावती की प्रेम-कथा के वर्णन द्वारा कवि ने अपने प्रेमतत्व के सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न किया है और इस बात का उन्होंने उक्त ग्रंथ के उपसंहार भान में स्पष्ट-रूप से उल्लेख भी कर दिया है, किंतु ध्यानपूर्वक देखने से पता चल जाता है कि अपने उच्च आदर्शों की ओर ही विशेष-रूप से उन्मुख रहने के कारण, वे बहुत कुछ घटाने-बढ़ाने पर भी, प्रेम-कहानी को उचित ढंग से निबाहने में भलीभाँति कृतकार्य नहीं हो सके है। प्रेम-कहानी में आए हुए ऐतिहासिक अंश तथा कवि के मनोगत सांप्रदायिक भावों ने भी इस की सफलता में, कदाचित्, बहुत कुछ बाधा पहुँचाई है। प्रथम के कारण, उद्देश्यनुसार जोड़ी गई नवीन बातों का बेमेल होना खटकता है तो द्वितीय के कारण, भावावेश में आकर कविद्वारा वर्णित योग-संबंधी बातों का यथास्थल प्रकट होता रहना अरुचिकर प्रतीत होने लगता है।
पद्मावत ग्रंथ में, अपनी प्रियतमा पद्मावती से भेंट करने के उद्देश्य से, विकट सिहलगढ़ पर विजय प्राप्त करने के इच्छुक, राजा रतनसेन को महादेव ने जो जो उपाय बतलाए है वे ठीक ठीक वही है जिन्हें एक योगी अपने शिष्य को समझाने के लिए रूपक का साधारण रंग देकर, बतला सकता था। वास्तव में कवि ने इसी स्थल पर आत्मदर्शनाभिलाषियों के लिए आत्मसाधन का उपदेश भी दे दिया है जो इसीलिए उन के प्रेमतत्व-साधना-संबंधी सिद्धांतों का सार-स्वरूप है। महादेव ने राजा रतनसेन से इस प्रकार कहा है-
गढ़ तस वकि जैसि तोरि काया।
पुरुष दखु ओही कै छाया।।
पाइय नाहिं जूझ हठि कीन्हे।
जेइ पाया तेइ आपुहिं चीन्हे।।
नो पौरी तेहि गढ़ मझियारा।
औ तहँ फिरहिं पाँच कोटवारा।।
दसवँ दुवार गुपुत एक ताका।
अगम चढ़ाव बाट सुठि बाँका।।
भेदै जाइ कोइ ओह घाटी।
जो लह भेद चढ़ै होइ चाँटी।।
गढ़ तर कुंड सुरँग तेहि माहाँ।
तहँ वह पंथ कहौं तेहि पाहाँ।।
चोर बैठ जस सेंधि सँवारी।
जुआ पैंत जस लाव जुआरी।।
जस मरजिया समुद्र धँस, हाथ आव तब सीप।
ढूँढि लेइ जो सरग-दुआरी, चढै सो सिंघलदीप।।
दसवँ दुवार ताल कै लेखा।
उलटि दिस्टि जो लाव सो देखा।।
जाइ सो तहां साँस मन बंधी।
जस धँसि लीन्ह कान्ह कालिंदी।।
तू मन नाथु मारि कै साँसा।
जो पै मरहि आपु करि नासा।।
परगट लोकचार कहु बाता।
गुपुत लाउ मन जासौं राता।
हौं हौं कहत सबै मति खोई।
जौं तू नाहिं आहि सब कोई।।
जियतहि जुरै मरै एक बारा।
पुनि का मीचु को मारै पारा।
आपुहि गुरु सौ आपहि चला।
आपुहि सब औ आपु अकेला।।
आपुहि मीच जियन पुनि, आफुहि तन मन सोइ।
आपुहि आपु करै जौ चाहै, कहाँ सो दूसर कोइ।।
अर्थात् हे राजा रतनसेन, यह सिंहलगढ़ उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार तुम्हारा शरीर है और यदि सच पूछो तो, यह उसी की एक छाया-मात्रा है। अतएव केवल हठ-पूर्वक युद्ध करने से ही इस पर विजय नहीं मिल सकती। इसे वही पा सकता है जिसे अपने आपकी पहचान हो जाय। इस गढ़ में नव दर्वाज़े है जिन पर पाँछ दुर्गरक्षकों का सदा पहरा पड़ता रहता है और इस में एक दसवाँ गुप्तद्वार भी है जिस पर चढ़ना अत्यंत कठिन है क्योंकि उस तक जानेवाला रास्ता बहुत ही टेढ़ा-मेढ़ा है। इस मार्ग को पार करने वाला केवल वही हो सकता है जो गढ़ के सारे भेदों का जानकार हो तथा जिसे चीटियों की चाल से चलना भी आता हो। गढ़ के ही नीचे एक कुंड से होकर उस द्वार तक एक सुरंग लगी हुई है, वही रास्ता है। इस लिए, चोर जिस प्रकार सेंध ठीक कर के अंदर घुसा करता है, जुआ खेलनेवाला दाँव लगाकर बाजी मारता है और समुद्र में डूबकर मरजिया सीप निकालता है, उसी प्रकार जो उक्त स्वर्गद्वार का पता पा लेगा वही सिंहलगढ़ पर चढ़ सकेगा। दशम द्वार, वास्तव में, ताड़ के समान ऊँचाई पर है इस लिए उलटी दृष्टि लगाने वाले ही उसे देख भी सकते है। वहाँ पर पहुँचनेवाला अपने मन एवं प्राणों को वश में करने पर ही जा सकता है। जिस प्रकार कृष्ण ने जमुना में कूदकर नाग नाथ लिया था उसी प्रकार तुम भी अपने प्राणों को रोक कर मन को जीत लो और अपने आप को सिद्ध कर लो। प्रकट में तो लोकाचार की बातें करते जाओ, किंतु गुप्तरूप से अपनी प्रियतमा पर सदा ध्यान लगाए रहा करो। मैं मैं कहते कहते तुम ने अपनी सारी बुद्धि खा दी है इस लिए तुम्हारे ममत्व छोड़ने पर ही सब कुछ हो सकेगा जीते जी जुट कर एक बार यदि अहंकार का नष्ट कर दोगे तो फिर मृत्यु अथवा मारने वाले की आवश्यकता ही न रह जायगी। तुम स्वयं गुरु और स्वयं शिष्य भी हो, स्वयं तुम अकेले सब कुछ हो। मृत्यु जीवन, शरीर अथवा मन सब तुम्हारे ही अंतर्गत है। अपने आप को जान लेने वाले के लिए कोई वस्तु बाहरी नहीं।
कहना न होगा कि उपरोक्त अवतरण में आत्मदर्शन के उद्देश्य से की जाने वाली योगसाधना का उपदेश स्पष्ट दीख पड़ रहा है। कहने को तो जायसी यहां पर सिंहलगढ़ की दुर्जयता एवं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए साधनों का उल्लेख करते जा रहे हैं, किंतु वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही रहने के कारण इन के वर्णन में वह स्वाभाविक नहीं दीखती और इन के सिद्धांतों का ज्ञान रखनेवाले को शीघ्र पता चल जाता है कि “आपुहि चीन्हे” से यहाँ कवि का अभिप्राय आत्मज्ञान से, “नौ पौरी” द्वारा नव ज्ञानेंद्रियों से, ‘पाँच कोटवारा’ द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद व मोह से, ‘दसवँ दुवार’ द्वारा ब्रह्मरंध्र से, ‘कुंड’ द्वारा कुंडलिनी से, ‘सुरंग’ द्वारा सुपुम्ना नाड़ी से, ‘साँस मन बँधी’ द्वारा प्राणायाम और मनो निग्रह से, “हौ हौ” कहत द्वारा अहंकार से तथा “जियतहि जुरै मरै एक वारा” द्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्त करने से है। इसी प्रकार “चढ़ै होइ चाँटी” से यहाँ तात्पर्य साधकों के पिपीलिका-मार्ग से जान पड़ता है तथा यह भी विदित हो जाता है कि कवि ने कुंड को ‘गढ़तर’ कह कर कुंडलिनी की स्थिति मूलाधार के निकट बतलायी है ‘दसँव दुवार’ को “ताल कै लेखा” कह कर ब्रह्मरंध्र के स्थान का संकेत मानव शरीर के सर्वोच्च प्रदेश अर्थात् शिरोभाग के भी ऊपर किया है तथा ‘आपुहि गुरु सो आपुहि चेला’ इत्यादि से लेकर ‘कहाँ सो दूसर होइ’ तक के उस कथन का उद्देश्य ‘एक मेकाद्वितीय ब्रह्म’ एवं ‘अहंब्रह्मास्मि’ अथवा ‘तत्वमसि’ का प्रतिपादन मात्र है। वास्तव में पद्मावत की प्रेम-कहानी और प्रेमतत्व का रहस्य ही कुछ ऐसा है। जायसी ने ‘अखरावट’ में कहा भी है-
कहा मुहम्मद प्रेम-कहानी।
सुनि सो ज्ञानी भये धियानी।।
अर्थात् जायसी द्वारा कथित प्रेम-कहानी को सुन कर तत्वज्ञानी लोग योगी हो जाते हैं।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.
