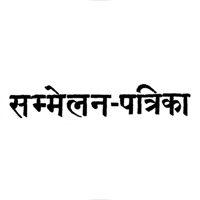सूफ़ी काव्य में भाव ध्वनि- डॉ. रामकुमारी मिश्र
भाव स्पष्टतः स्थायी भावों से सम्बद्ध हैं किन्तु विभावों की सम्यक् योजना न होने पर भी वे प्रयुक्त हो सकते हैं अतः अनुभवों के आधार पर अथवा चित्तवृत्तियों की प्रधानता के अनुसार भाव ध्वनियों का निर्णय समीचीन प्रतीत होता है। सूफ़ी काव्यों (14-16वीं शती के) में प्राप्त भाव ध्वनियों के स्थलों की संख्या काफी बड़ी है। (कुल 215 स्थल)। हमने भावों की एकरूपता के अनुसार इन्हें 27 वर्गों में विभाजित किया है। यह विभाजन सर्वमान्य 33 संचारी भावों से कुछ भिन्न है। किन्तु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि हमने जानबूझ कर अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया है। हमारे विचार से भावों का वर्गीकरण प्राप्त सामग्री के आधार पर ही यथोचित ढंग से हो सकता है। भावों के नामकरण के पचड़े में न पड़ कर यथातथ्य अंकित करना हमने श्रेयस्कर समझा है। भोज द्वारा निर्दिष्ट अनुरागों को हम भावों के सर्वाधिक निकट पाते हैं। हमारे द्वारा प्रस्तावित भावों का वर्गीकरण निम्नांकित प्रकार है (उनके सम्मुख प्राप्त स्थलों की संख्यायें अंकित हैं)-----
1. वात्सल्य 24
2. प्रकृति प्रेम 9
3. प्रेम, प्रीति, रति 8
4. विरह, विवाद, पश्चात्ताप, संताप, शोक, विलाप, निरुत्साह, उदीसनता 21
5. हर्ष, प्रसन्नता 10
6. चिन्ता, शंका, आशंका 6
7. अभिलाषा, आकांक्षा, उत्सुकता, उत्कंठा, आशा (निराशा भी), पूर्वानुमान, शकुन 24
8. स्मरण 3
9. मोह, जड़ता, मूर्छा, स्वप्न 13
10. तिरस्कार, अनादर, अपभाव, वर्जना 3
11. विनम्रता, विनयशीलता, दीनता, दैन्य, अनुनय-विनय, आदर, स्तुति, भक्ति 14
12. चाटुकारिता, प्रशंसा 4
13. वीरोक्ति, देश प्रेम, प्रोत्साहन, उद्बोधन, आह्वान 9
14. पातिव्रत्य, अनुरक्ति, निष्कलुषता, निष्ठा, न्याय 15
15. कपट 1
16. समता, सौहार्द, सहृदयता, मित्रता 8
17. तादात्म्य 5
18. वितर्क 9
19. विकल्प 2
20. क्रोध, उग्रता 2
21. भय, त्रास 5
22. आश्चर्य 5
23. व्यंग्य (हास्य) 3
24. करुणा 2
25. घृणा 1
26. आशीष 3
27. लज्जा 5
इनमें से वात्सल्य, प्रकृति, प्रेम-प्रीति, रति-ये तीनो श्रृंगार रस से सम्बद्ध है। वीरोक्ति, देश-प्रेम आदि (13 वाँ वर्ग) वीर रस से, पातिव्रत्य, समता आदि (वर्ग 14, 16) श्रृंगार तथा शान्त रस से, क्रोध, उग्रता रौद्र रस से, आश्चर्य, अद्भुत रस से, व्यंग्य हास्य रस से, करुणा करुण रस से, घृणा वीभत्स रस से सम्बन्धित भाव ध्वनियाँ है।
इन भाव ध्वनियों में से कुछ तो पाँचों सूफ़ी काव्य कृतियों में समान रूप से पाई जाती है, कुछ केवल चार में, कुछ तीन, कुछ दो और कुछ केवल एक-एक कृति में पाई जाती है। इस दृष्टि से भाव ध्वनियों को निम्नांकित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है।
पाँचों कृतियों में समान रूप से प्राप्तः प्रेम, प्रीति, विरह, अभिलाषादि, पतिव्रत्यादि
चार कृतियों में समान रूप से प्राप्तः वात्सल्य, प्रकृति, विनम्रतादि, वीरोक्ति, वितर्क, लज्जा।
तीन कृतियों में समान रूप से प्राप्तः हर्ष, प्रसन्नता, स्मरण, भय, त्रास, व्यंग्य।
दो कृतियों में सामन रूप से प्राप्तः जड़ता, मोहादि, चाटुकारितादि, समतादि, तादात्म्य, विकल्प, क्रोधादि, आश्चर्य, आशीष।
केवल एक कृति में प्राप्तः तिरस्कार (चन्दाधन), कपट (माधवानल), करुणा (माधवानल), घृणा (मृगावती)।
समस्त भाव-ध्वनियों में वात्सल्य, विरहादि, अभिलाषादि के उदाहरण सर्वाधिक है। इन भाव ध्वनियों में कुछ विरोधी भावों से जन्य हैं- यथा वर्ष 11 तथा 12। कुछ भाव ध्वनियाँ सर्वथा नवीन हैं- यथा तादात्म्य, पतिव्रत्य, निष्ठा तथा समतादि। हमने वात्सल्य या वत्सलता को रस न मान कर भाव माना है। इसी प्रकार प्रकृति-प्रेम को भी हमने भाव मानना उचित समझा है। प्रेम, प्रीति, रता तथा विरह-विषाद यद्यपि श्रंगार रस के संयोग तथा विप्रलम्भ श्रृंगार में अन्तर्भूत किए जा सकते हैं किन्तु भावों की विविधताओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन्हें पृथक्-पृथक् रखा गया है।
अब हम भाव ध्वनियों की विवेचना कतिपय महत्वपूर्ण स्थलों को उद्धृत करते हुए करेंगे किन्तु पूर्णता की दृष्टि से विभिन्न कृतियों में प्राप्त स्थलों का भी उल्लेख किया जाएगा।
1. वात्सल्य भाव ध्वनि
वात्सल्य भाव ध्वनि कई प्रकार से अभिव्यक्त हुई है----
1. सन्तान के प्रति माता-पिता का प्रेम अथवा माता-पिता के प्रति सन्तान का प्रेम।
2. सन्तानों में परस्पर प्रेम।
3. धाई, सन्देशवाहक या अन्यों द्वारा माता-पिता वात्सल्य भाव ध्वनियों को हल निम्नांकित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं----
(क) माँ का बेटे के लिए पक्षपातः यथा बावन की माँ चाँद को बुरा कहती है, बावन को नहीः
बावन मोर दूध कर पीवा, निस कित बावन तो संग सोवा।
तूं अमरैल न देखसि काहू, बिन धहि बस नवइ गयाहू।।
चंदायन 49.3-4
(ख) भाई बहन का प्यारः प्रेमा का राजकुमार के प्रति भाई का-सा प्यार प्रदर्शित करना।
मैं मधुमालती राजकुमारी, संतत आउ संघ महतारी।
कुँअर जाहु जौ चितबिआऊं, हम घर जाहि लेहु सुह नाऊं।।
भाई बहिन पिता महतारी, करिहै भगति अनेग तुम्हारी।
मधुमालती, 251.3-5
(ग) माता के निर्दयी होने पर सन्तान द्वारा कुशब्द कथन- चिड़िया बना देने पर मधुमालती का अपनी माँ के लिए कुशब्द कहनाः
डाइनि पुनि जग धीज न खाई- मधुमालती, 381.5
(च) माता पिताः पुत्र सेः जोग उतारने को कहना, कष्ट मिलने का भय दिलाना।
कहहिं पूत तें आस हमारी, राज छोड़ कस होहु भिखारी।
और अहै जो अरब भंडारा, अब लगि मैं तोहि लागि संभारा।।
जो तुह काज न आवे आजू, सो मेरे पुनि कवने काजू।।
मधुमालती, 172.3-5
बिनवे रतनसेनि कै माया, मांथे छत्र पाट निति पाया।
बेरसहु नौ लखि लच्छि पियारी, राज छाड जनि होहु भिखारी।।
निति चंदन लागै जेहि देहा, सो तन देखु मरब अब खेहा।
सब दिन करत रहेउ तुम्ह भोगू, सो कैसे साधन तप जोगू।।
-पद्मावत, 129.1-4
(ङ) पुत्र का माता पिता से हठ या अनुरोधः (आज्ञाकारिता भी अन्तर्निहित है)
मोहि यह लोभ सुनाउ न माया, काकर सुख काकरि यह काया।
जौ नियान तन होइहि छारा, माँठि पोखि मरै को भारा।।
-पद्मावत, 130.1-2
यह अपनी माँ से रत्नसेन का अनुरोध है।
चरन लागि मांगौं कर जोरी, सुनहु पिता यह बिनती मोरी।
बिनु जिव कहहु कह जाई, जिउ तेहि पहं गयां गई लखाई।।
साथ गये तुम्हरे दुख पइहौं, हिव फाटी ततखन मरि जइहौं।।
मृगावती, 23.1-3
यह अपने पिता से राजकुमार का अनुरोध है।
(च) पुत्र या पुत्री का कथन धाई सेः अपनी व्यथा सुनाने, सन्देश कहने, आत्मीयता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से।
माइ मोर तोह धाइ न होहू, तोहिं छांडि यह उठै मोरांहू।
ताकर रूप कहौं मैं तोहीं, बैठे समुझि टेक देहु मोही।।
-मृगावती, 31.1-4
यह राजकुमार का कथन धाई से है।
धाई दोख न अहै किछ तोरा, कहेहु जोहार कुँवर से मोरा।
-मृगावती, 60.1
(छ) धाई स्नेहः मृगावती के अदृष्ट हो जाने पर राजकुमार की दशा देख करः
धाय आई जो देखै पासा, मुझ में भरत न आह न साँसा।
अमिअ सौंधि बैठाल संभारी, काह देख तें गा बिसंभारी।।
-मृगावती, 30.4-5
(ज) सास-ससुर से भी वत्सलता को प्राप्तिः ताराचंद तथा राजकुमार के वचन प्रेमा तथा मधुमालती के माँ-बाप से।
मीत हम जन्मे हो बारा, माघ जाप जे तुह प्रतियारा।
महि परिवार गोसाइनि रानी, विसर तरै इन्ह अँजुरिन्ह पानौ।।
मधुमालती, 524.2-3
(झ) माँ का पश्चातापः मधुमालती को पक्षी बनाकर उस पर निर्दयता करने के लिए।
तौ पिंजरा उर लावा धाई, देखी दुहिता न रही रोवाई।
खन खन गेरै निरखै बारी, नैन नीर नहिं रही पनारी।।
मधुमालती, 393.1-2
2. प्रकृति प्रेम
यद्यपि इसे श्रृंगार रस के अन्तर्गत उद्दीपन विभाव के रूप में रखा जा सकता है किन्तु हमने इसे भाव माना है। इसके प्रमुख अंग हैं मानवीकरण, उल्लास एवं उत्साह। इसका सम्बन्ध प्रकृति के साहचर्य से है और यह चित्त के विकास को प्रदर्शित करता है। विवेच्य सूफी काव्यों में प्रकृति प्रेम सम्बन्धी भावों को हम दो प्रकार से विभाजित करके उनका वर्णन कर सकते हैं।
अ) प्राकृतिक दृश्यों के यथातथ्य वर्णनः इसके अन्तर्गत मनुष्य के प्राकृतिक दृश्यों के प्रति अनुराग- यथा (क) जल, ताल, मानसरोवर के वर्णन या (ख) अँबराई, मधुवन के वर्णन को सम्मिलित किया जा सकता है- चन्दायन (22.1), मृगावती (93.4-6), पद्मावत (31.1-9, 33.1-7)) में प्रथम प्रकार (क) की तथा पद्मावत (29.1-9), मधुमालती (201.2-5) में द्वितीय प्रकार की भावध्वनि प्राप्त होती है। इसके केवल एक-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे।
तालाब वर्णनः पैरहिं हंस माछु बहिराहें, चकवा चकई केरि कराहैं।
दबला ढेंक बैठ झरपाये, बगुला बगुली सहरी खाये।।
-चंदायन, 22.1-2
जल वर्णनः सीतल सेत अंबुकर रूपा, एक कपूर जो सुनहु अनूपा।
फूले पुहुप कंवल तहँ अहा, लुबुधा भँवर पेम कर गहा।।
-मृगावती, 93.3-4
मानसरोवर वर्णनःफूला कँवल रहा होइ राता, सहस सहस पंखुरिन्ह कर छाता।
उलथहिं सीप मोति उतिराहीं, चुगहिं हंस औ केलि कराहीं।
कनक पंखि पैरहिं अति लोने, जानहु चित्र सँवारे सोने।।
-पद्मावत, 31. 5-7
(आ) ऋतु वर्णनः वसंत तथा वर्ष ऋतु के वर्णन-
वसंतः-
आज वसंत नवल रितु राजा, पंचमि होइ जगत सब साजा।
नवल सिंगार बनाफति कीन्हा, सीस परासन्ह सेंदुर दीन्हा।
बिगसि फूल फूले बहु बासा, भँवर आइ क्षुबुधे चहुँ पासा।
-पद्मावत, 183.4-6
वर्षाः
छठ भावो सिद्धि भइ अंधियारी, नैन न सूझै बाँह पसारी।
खिन बरजै फिर दहव बरीसा, खोर भरे जर बाट न दीसा।
दादुर ररहिं बीजु चमकाई, एइस न जानि कवनु दिसि जाई।
-चंदायन, 200.1-4
3. प्रेम, प्रीति, रति भाव ध्वनि
यद्यपि भोज ने 64 अनुरागों के अन्तर्गत इनका सूक्ष्म विभेद उदाहरणों द्वारा अंकित किया है किन्तु हम इन्हें एक ही प्रकार के भाव से सम्बद्ध मानते हैं। इनमें केवल भावात्मक भेद हो सकता है या प्रकारों का। इनमें मूल भाव एक ही है।
कुसुम चीर तर देखेउं फरे बेल इह भांत।
राजा खाइ बिसरिगा, सुन अस्थन भइ सांत।।
-चंदायन, 88.6-7
(यहाँ बेल के समान कठोर कुचों के वर्णन से प्रेम एवं रति भाव की उत्पत्ति होती है)
मैं आपन जिउ ताहियइ काढ़ा, प्रेम प्रीति रस जेहि दिन बाढ़ा।
पेम लागि मैं जिउ परद्देवा, भौंर मरै पै छाँड न केवा।।
-मृगावती, 186.4-5
(अनुरक्ति जताते हुए प्रेम भाव की पुष्टि)
कैसेहुं नवहिं न माएं, जोबन गरब उठान।
जौ पहिले कर लावै, सो पाछे रति मान।।
-पद्मावत, 483.8-9
(कुचों की उन्नति से आकृष्ट होना- प्रेम एवं रति ध्वनि)
4. विरह विधादावि भाव ध्वनि
इन स्थलों में प्रायः विरह शब्द पाया जाता है, अतः स्वशब्द वाच्यत्व के कारण रसदोष है किन्तु उनमें विरह ध्नवि तो है ही।
विरहः-रकत न आवा दीख न धाऊ, हिए साल मोर उठे न पाऊ।
-चंदायन, 96.9
राजा इहां तैस तपि भूरां, भा जरि विरह छार कर कूरा।
-पद्मावत, 235.1
विवादः
दइया कौन मैं कीन्ह बुराई, सरें कचौंर बूडेउं आई।
-चंदायन, 45.5
रोवै बहुत बात नहिं आवै, सौंरि साँरि पछिताय।
-मृगावती, 20.7
भयनिश्चित विवादः
कहै काह मैं मुख देखराउव, खन एक माहं कुँवर जो आउब।
-मृगावती, 58.5
(.....................................उपलब्ध नहीं है।)
(5 और 6 शीर्षक उपलब्ध नहीं है।)
7. अभिलावाद्धि ध्वनि
ये भाव ध्वनियाँ चिन्ता से भिन्न हैं। रूपाकर्षण जन्य उत्सुकता, उत्सर्ग से युक्त अभिलाषा, पूर्वाभास, शकुन आदि मनोवांछित फल की प्राप्ति –ऐसी भाव ध्वनियाँ इस वर्ग में सम्मिलित है। निराशा इस वर्ग की ध्वनियों की विलोभ ध्वनि हैं। यह माधवानल (51.4-5) में पाई गई है।
रूपाकर्षण अन्य उत्सुकताः
चाँदा का नाम सुनकर राव का आसक्त होना।
बाजिर कौन देस सौ नारी, ठौर कहउ बरु तुमहि बिचारी।
करन कहउ औ लखन बिसेखी, अछरी रूप सो तिरिया देखी।।
मारग कौन कैस बेवहारा, लांब छोट कस आह------
-चंदायन, 74. 4-6
दई विधाता पूजइ आसा, अस तिरिया जो पावइ पासा---
-चंदायन, 305.2
रातिगु देवस इहै मन मोरे लागौं कंत छार जेंउ तोरे-
-पद्मावत, 352.7
विधि सो देवस कब होइहि मोरा, जो देखब ससि बदन इंजोरा।
-मधुमालती, 244.5
निष्ठा से युक्त अभिलाषाः
सौ पदुमावती गुरु हौं चेला, जोग तंत जेहि कारन खेला।
तजि ओहि बार न जानौं दूजा, जेहि बिन मिले जातय पूजा।।
=पद्मावत, 246. 1-2
सम्भावनाः
जो विधि इन्ह दुहुं होइ मेरावा,
बाजै तीनो लोक बचावा -मधुमालती, 69.2
............. मिलन औचि सुनि जिउ गहवरा,
दौरि कुँवर पेमा पाँव परा।
-मधुमालती, 296.1
आशाः
पंडित वैद बिदेसिया, गुनी सो सुंदर आहि।
सनमुख आवत देखि कै, रहीं सखीं सब चाहि।।
-माधवानल, 134. 6-7
शकुनः
कहा आजु अस सगुन जनावा, हरखि हरखि जे गहवरि आवा।
फरकै नैन मुआ बर मोरा, पान पियार आव कोउ कोरा।।
-मधुमालती, 281.2-3
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.