महाकवि माघ और उनका काव्य सौन्दर्य- श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री
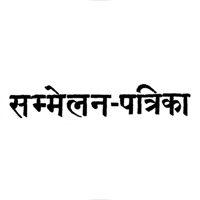
महाकवि माघ और उनका काव्य सौन्दर्य- श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री
सम्मेलन पत्रिका
MORE BYसम्मेलन पत्रिका
माघ केवल एक सिद्धहस्त कवि ही नहीं थे, प्रत्युत वे एक सर्वशास्त्रतत्वज्ञ प्रकाण्ड पण्डित भी थे। उनकी जैसी बहुज्ञता तथा बहुश्रुतता अन्य संस्कृत कवियों में कम मिलती है। भिन्न-भिन्न शास्त्रों की छोटी-से-छोटी बातों का जिस निपुणता एवं सुन्दरता के साथ उन्होंने वर्णन किया है, उससे ज्ञात होता है कि उन सब पर उनका असाधारण अधिकार था। संस्कृत साहित्य के किसी अन्य काव्यग्रन्थ में विविध शास्त्रीय एवं लौकिक विषयों पर इस प्रकार साधिकार रचना करने की सफलता अकेले माघ को ही मिली थी। दर्शन, राजनीति, कूटनीति, सामाजिक जीवन, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, सेना, गज एवं अश्व-शास्त्र तथा युद्धविज्ञान, मंत्र, पुराण, गाथा, वर्णाश्रम मर्यादा, अलंकार एवं छन्द-शास्त्र- इन सब पर उनका यथेष्ट अधिकार था। यद्यपि वे सनातन धर्मानुयायी थे किन्तु नास्तिक दर्शनों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों की भी उन्हें अच्छी जानकारी थी और उन सब पर पूर्ण सहानुभूति भी थी। वेदों से लेकर पुराणों एवं स्मृतियों तक पर उनका पूर्ण अधिकार था, साथ ही व्याकरण के तो वे प्रकारण्ड पण्डित ही थे। पुरोहित-कर्म एवं यज्ञ-दीक्षा आदि कर्मकाण्डो के सम्बन्ध में भी उनकी जानकारी एक अधिकारी विद्वान की थी। नीचे कतिपय उदाहरणों द्वारा उनके इन सभी विषयों के असाधारण पाण्डित्य पर प्रकाश डाला जायगा।
आस्तिक दर्शनों में से यथावसर उन्होंने जो प्रसंग लिये है, उन्हें अच्छी तरह पल्लवित भी किया है। विशेषकर साख्य के तत्वों की चर्चा तो उन्होंने अनेक स्थलों पर की है। इसी प्रकार बौद्ध दर्शन की कुछ बातों की भी अनेक स्थलों पर चर्चा की गयी है। प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद ने भगवान् श्रीकृष्ण की जो प्रार्थना की है वह साख्य शास्त्र के अनुसार है। इसी प्रकार चौदहवें सर्ग में राजसूर्य यज्ञ के प्रकरण में सांख्य मत की उपमा देते हुए युधिष्ठिर के लिए बताया है कि वे स्वयं कुछ कार्य नहीं कर रहे थे- पुरोहित ही उनका सब कार्य कर रहे थे।
उदासितारं निगृहीत मानसैर्गृहीतमध्यात्मदृशा कथञ्चन।
बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः।।
तस्य सांख्य पुरुषेणतुल्यतां विभ्रतः स्वयंमकुर्छतः कियाः।
कर्सता तदुपलम्भतोअभवद् वृत्तिभाजि करणे यथर्त्विजि।।
मीमांसा और वैशेषिक दर्शन की चर्चा भी इसी राजसूर्य यज्ञ के प्रसंग में की गयी है और उनके सिद्धांतों का विश्लेषण भी हुआ है। चौदहवें सर्ग में राजसूर्य यज्ञ के प्रकरण में व्याकरण, वेद, कर्मकाण्ड एवं दान की छोटी-छोटी बातों की चर्चा की गयी है। उनसे मालूम पड़ता है कि कवि ने अपने जीवन में किसी विशाल यज्ञ का समारम्भ एवं समारोह सम्पन्न किया था। राजसूर्य यज्ञ में दान के मार्मिक प्रसंगों को लेकर कवि ने अपनी सहृदयता से अत्यन्त उज्ज्वल तो बना ही दिया है, साथ ही युधिष्ठिर के पाव-चरित में भी चार चाँद लगा दिया है। नीचे के श्लोक देखिएः-
निर्गुणोअपि विमुखो न भूपतेदनिशौण्डमनसः पुराभवत्।
वर्षकस्य किमयः कृतोन्नतेरम्बुदस्य परिहार्यमूषरम्।।
प्रेम तस्य न गुणेषु नाधिकं न स्म वेद न गुणान्तरं च सः।
दित्सया तदपि पार्तिवोअर्थिनं गुण्य गुण्य इति न व्यजीगणत्।।
सर्ग 14।46,47।।
इसी प्रकार योगशास्त्र विषयक प्रवीणता के लिए कवि के निम्नलिखित दो श्लोक पर्याप्त है।
मैत्र्यादि चित्त परिकर्म विदो विधाय क्लेशप्रहाणमिह लब्ध सबीज योगाः।
ख्याति च सत्व पुरुषान्यतयाअधिगम्य वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो निरोद्धुम्।। सर्ग 4।54
सर्व वेदिनमनादिमास्थितं देहिनामनुजिघृक्षया वपुः।
क्लेश कर्म फल भोग वर्जितं, पुं विशेषममुसीश्वरं विदुः।।सर्ग 14।62
प्रथम श्लोक में प्रयुक्त मैत्र्यादि, चित्त परिकर्म्, सबीजयोग, सत्व पुरुषान्य तयाख्याति, क्लेश आदि योगशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली हैं तथा द्वितीय श्लोक में योगशास्त्र के सिद्धान्तों की दृष्टि से परमात्मा की विशिष्ट संज्ञाओं अथवा विशेषणों की चर्चा की गयी है। यहाँ ज्ञानी पुरुष से कवि का तात्पर्य योगी पुरुष से है।
अद्वैत वेदान्त के तत्वों का प्रतिपादन तो अनेक स्थलों पर है। संसार को मिथ्या माया मान कर ब्रह्म अथवा परमात्मा को ही एकमात्र सत्य मानने की चर्चा तथा केवल ब्रह्म-ज्ञान प्राप्ति की साधना एवं मोक्ष-प्राप्ति की आकांक्षा को कवि ने अनेक स्थलों पर प्रकट किया है। वेदान्त की कुछ अन्यान्य सिद्धान्त-परक बातों की भी न-उन अवसरों पर चर्चा आयी है। इस सम्बन्ध में एक ही प्रसंग उद्धृत कर देना पर्याप्त है।
ग्राम्य भावमयहातुमिच्छवो योगमार्गपतितेन चेतसा।
दुर्गमेकमपुनर्निवृत्तये यं विशन्ति वशिनं मुमुक्षवः।।14 सर्ग।64।।
नास्तिक दर्शनों में बौद्धमत की चर्चा अनेक अवसरों पर ही की गयी है तथा जैन मत के आदि प्रवर्तक महावीर स्वामी के प्रति भी एक स्थान पर आदर व्यक्त किया गया है। जहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कवि ने पुराणवादियों की भाँति महावीर स्वामी को भी भगवान् विष्णु का एक अवतार स्वीकार किया है।
सर्व कार्यशरीरेवु मुकतवाअङ्गस्कन्ध पञ्चकम्।
सौगतानामिवात्माअन्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम्।।सर्ग 2।26।।
इस एक ही श्लोक में कवि ने बौद्ध दर्शन की स्थूल बातों के साथ राजनीति की सूक्ष्म बातों की सुन्दर चर्चा कर दी है। मीमांसा शास्त्र की निपुणता निम्नलिखित दो श्लोकों से ज्ञात होती है।
प्रति शरणमशीर्ण ज्योतिरग्न्यताहितानां विधिविहित विरिब्धैः सामिधेनौरधीत्य।
कृतु गुरु दुरितौघ ध्वंसमघ्वर्युवयैं र्हुतमयमुपलीढे साधु सानाय्यमग्निः।।सर्ग 11।41।।
शब्दितामनपशब्द मुच्यकैर्वाक्य लक्षण जिदोअनुवाक्यया।
याज्यया यजन धर्मिणोअत्यजन् द्रव्यजातमयदिश्य देवताम्।।सर्ग 14।20।।
संगीत एवं अन्यान्य उपयोगी ललित कलाओं की सूक्ष्म बातों की चर्चा अनेक जगह की है। गायन, वाद्य, स्वर, ताल, लय आदि के सम्बन्ध में कवि की अधिकारपूर्ण उपमाएं एवं उक्तियां सिद्ध करती है कि संगीत-शास्त्र पर उसका साहित्य-शास्त्र के समान ही असाधारण अधिकार था। इसी प्रकार नृत्यकला तथा नाटयकला पर भी उसने अधिकार प्राप्त किया था। कवि की संगीत की निपुणता निम्नलिखित दोनों श्लोकों से प्रकट होती है-
रणदिभराघट्टनया नभस्वतः पृथग्विभिन्न श्रुतिमण्डलैः स्वरैः।
स्फूटीभवद् ग्राम विशेष मूर्च्छनामवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः।।सर्ग 1।10।।
श्रुति समधिकमुच्यैः पञ्चमं पीडयन्तः सततमृषभहीनं भिन्नकीकृत्य षड्जम्।
प्रणिजगदुरकाकु श्रावकस्निष कष्ठाः परिणतिमिति रात्रेमगिधा माधवाय।।सर्ग 11।1।
नीचे के श्लोकों में श्लेष की सुन्दर छटा के साथ-साथ कवि ने अपने नाटयशास्त्रीय ज्ञान का जो परिचय दिया है, वह उच्च कोटि का है-
दधतस्तनिमानमानुपूर्व्या वभुरक्षिश्रवसो मुखे विशालाः।
भरतज्ञ कवि प्रवीतकाव्यग्रथितांका इव नाटक प्रपंचाः।।सर्ग 20।44।।
तथा स्वादयन रसमनेकसंस्कृत प्राकृतैरकृतपात्र संकरैः।
भावशुद्धि विहितैर्मुदं जनो नाटकैरिव वभार भोजनैः।।सर्ग 14।50।।
कवि की राजनीतिज्ञता के सम्बन्ध में तो उसके अकेले महाकाव्य के उद्धरणों से एक छोटी-मोटी पुस्तिका प्रस्तुत की जा सकती थी। राजा के छोटे-मोटे कर्तव्यों से लेकर उसकी सेना की छोटी-छोटी बातों तक का उसे पूरा पता था। सन्धि-विग्रहादि गुणों के प्रयोगों के अवसरों पर उसने अपनी युक्तियों तथा परस्पर विरोधी तर्कों से उन्हें इतना सुगम बना दिया है कि उसकी सूझ-बूझ पर विस्मित होना पड़ता है। उद्धव और बलराम के मुख से तथा युधिष्ठिर और भीष्म के मुख से भी उसने राजनीति की जटिल से जटिल समस्याओं पर ऐसे उपादेय हल प्रस्तुत किये हैं, जो आज प्रजातन्त्र के युग में उसी प्रकार से प्रयोग में लाये जा सकते हैं। प्रजा की सर्वविध हितरक्षा और राजा के विशेष व्यापक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उसने जिस राजतंत्र की समर्थिका राजनीति की चर्चा अपने महाकाव्य में की है, वह भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की परम्परा के सर्वथा अनुकूल ही है। राजनीति की जटिल गुत्थियों पर उसने जो प्रसंगगत विचार प्रकट किये हैं, उससे ज्ञात होता है कि उसका यह ज्ञान कोरा किताबी ज्ञान नहीं था। शिशुपाल वध का द्वितीय सर्ग कवि की राजनीतिज्ञता का अच्छा निदर्शक है। राजनीतिक दाँव-पेचों की ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं छूटने पायी है, जिसकी कमी की ओर हमारा ध्यान जा सके। परस्पर विरोधी विचारों को आमने-सामने रख कर उसने उचित पक्ष के निर्णय का जो प्रसंग उपस्थित किया है, उससे पाठकों को भी दैनिक कार्यो में आवश्यक राजनीति का अपेक्षित ज्ञान हो जाता है। नीचे के कुछ श्लोकों में कवि की राजनीतिज्ञता का नमूना लीजिए-
सम्पदा सुस्थिरं मन्ये भवति स्वल्पयाअपि यः।
कृतकृत्यो विश्रिर्मन्ये न वर्धयति तस्य ताम्।। 2।32।।
विपक्षमखिली कृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा।
अनीत्वा पंकतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते।। 2।34।।
बिधाय वैरं सामदे नरोअरौ य उदासते।
प्रक्षिप्योदचिंषं कक्षे शेरते तेअभिमारुतम्।। 2।42।।
पादाहतं यदुत्थाय मूर्द्धानमधि रोहति।
स्वस्यादेवापमानेअपि देहिनस्तद्वरं रज।।।2।46।।
राजनीति के पारिभाषिक शब्दों का तो कवि ने अनेक अवसरो पर प्रयोग किया है, छः गुण, तीन, शक्ति, तीन उदय तथा अंग पंचक आदि पारिभाषिक शब्दों की चर्चा इन श्लोकों में देखिए-
षड्गुणाः शक्सयस्तिस्रः सिद्धयश्चोदयास्त्रयः। सर्ग।2।26।।
सर्व कार्य शरीरेषु मुक्त्वांगस्कन्धपञ्चकम्।। सर्ग2।28।।
कुछ दूसरे पारिभाषिक शब्दों को लीजिए-----
उदेसुमत्यजन्नीहां राजसु द्वादशस्वपि।
जिगीषुरेको दिनकुदादित्येष्विव कल्पते।। 2।81।।
बुद्धिशस्त्रः प्रकृत्यंगो घनसंवृति कञ्चुकः।
चारेक्षणो दूतमुखः पुरुषः कोअपि पार्थिवः। 2।82।।
सेना के विभागों तथा उपविभागों के साथ-साथ दुर्ग-रचना, अभियान, युद्धकला अथवा शस्त्रास्त्रों की मारपीट के अच्छे-अच्छे गुर कवि को वखयी ज्ञात थे। अठारहवें, उन्नीसवें तथा बीसवें सर्ग के 279 श्लोकों में कवि के इस विषय के परिपक्व ज्ञान का पूर्ण परिचय मिलता है। गजो और अश्वो के लक्षणों से लेकर उनके स्वभाव की छोटी से छोटी बातों की चर्चा कवि न की है। युद्धस्थल का ऐसा रोमाचकारी विपुल वर्णन संस्कृत काव्यों में अन्यत्र दुर्लभ है। खच्चरों और ऊँटोंसे लेकर बैलों और भैसों के स्वभावों तथा कार्यो की भी चर्चा की गयी है। साथ ही युद्धस्थल के लिए इन सब के खाद्य पदार्थों तथा उपयोगी औषधियों की भी अच्छी चर्चा है। अश्वों तथा गंजो के भेदों तथा गुण दोषों की भी उसे प्रामाणिक जानकारी रही। नीचे के दो श्लोकों में उसने अश्वो के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह उसके शालिहोत्री होने का पर्याप्त प्रमाण है----
तेजो निरोध समता वहितेन यन्त्रा सम्यक् कशात्रय विचार विदा नियुक्तः।
आरट्टजश्चटुलनिष्ठुरपातमुच्चैश्चित्रं चकार पदमर्श्रपुलायितेन।।5 सर्ग 10।।
तथा---
अव्याकुलं प्रकृतिमुतरधेयकर्मधाराः प्रसाधयितुमव्यतिकीर्ण रूपाः।
सिद्धं मुखे नवसु वीथिषु कश्चिदश्वं वल्गाविभागकुशलो गमयाम्बभूव।।सर्ग 5।60।।
इसी प्रकार हाथियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन श्लोक उसके गज-सम्बन्धी गहरे ज्ञान का विशेष परिचय देते हैं------
गण्डूष मुज्झितवता पयसः सरोषं नागेन लब्ध परवारण मारुतेन।
अम्भोधिरोधति पृथु प्रतिमानभागरुद्धोरुदन्त मुसलप्रसंरं निपेतें।।सर्ग 5।36।।
स्तम्भं महान्तमुचितं सहसा मुमोच दानं ददावतितरां सरसाग्रहस्तः।
बद्धापराणि परितो निगडान्यलावीत् स्वातन्त्र्यमुज्ज्वलमवाप केरुणुराजः।।
जज्ञे जनैर्मुकुलिताक्षमनाददाने संरब्ध हस्तिपकनिष्ठुरचोदनाभिः।
गम्भीरवेदिनि पुरः कवलं करीन्द्रे मन्दोअपि नाम न महानवगुह्य साध्यः।।
सर्ग 5।48-49।।
ऊँटों तथा जंगली सांड़ों और बैलो की प्रकृति का कवि ने इतना स्वाभाविक और सुन्दर वर्णन किया है कि उसमें रेखाचित्र प्रस्तुत करने की पूर्ण क्षमता है। दूध दुहते हुए गोपों, खेत की रखवाली करनेवाली गृहस्थ-रमणियों, हाथी, घोड़ा, ऊँट और खच्चर हाँकने वाले राजकर्मचारियों के चित्रण में एवं उनकी विभिन्न चेष्टाओं के वर्णन में कवि ने चित्रकार को भी चुनौती दे दी है। सचमु कवि के वर्णनों में रेखाओं के बिना चित्र प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण समाग्रियां मौजूद है। इन बातों से यह भी पता लगता है कि उसका चित्रकला पर भी अच्छा अधिकार था। एकाध स्थलों पर चित्रकला सम्बन्धी स्फुट प्रसंगों की चर्चा कर के कवि ने अपने इस विषय के ज्ञान का भी परिचय दिया है।
और कवि के साहित्य के विभिन्न अंगों- रस-सिद्धान्त, छन्द और अलंकार की सिद्धहस्तता का कहना ही क्या है? यह सब तो कवि का अपना अधिकृत क्षेत्र है। जिधर से उसकी इच्छा हुई है, प्रसंग आरम्भ किया है और जिधर से चाहा है, समाप्त किया है। राजनीति और कूटनीति जैसे नीरस विषयों में भी उसने साहित्यिक पदार्थों की चर्चा कर के उन्हें हृदयंगम करने योग्य और अधिकारिक उपादेय बना दिया है। नीचे के दो श्लोको में कवि ने अपने इस विषय के हस्तलाघव का अनुसरणीय प्रदर्शन किया है-----
तेजः क्षमाः वा नैकान्तं कालज्ञस्य महीपतेः।
नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवें।। 2।83।।
नालम्बते दैष्टिकतां न निजीवति पौरुषे।
शब्दार्थौ लत्कविरिन द्वयं विद्धानपेक्षते।।2।86।।
स्थायिनोअर्थे प्रवर्तन्ते भावाः सञ्चारिणो यथा।
रसस्यैकस्य भूयांसस्तथा नेतुर्महीभुतः।। सर्ग 2।87।।
आयुर्वेद अथवा वैद्यक शास्त्र की सिद्धान्तसम्बन्धी छोटी-मोटी बातों की चर्चा कवि ने अनेक अवसरों पर की है। उन सब के परिशीलन से ज्ञात होता है कि आयुर्वेद की रोग एवं औषधियों-सम्बन्धी अनेक बातों का उसे ज्ञान था, और कतिपय रसायनों तथा औपचारिक प्रयोगों की भी उसे पूरी जानकारी थी।
माघ के परम वैयाकरण होने की चर्चा पहले की जा चुकी है। अपने महावैयाकरण के रूप को उन्होंने प्रायः प्रत्येक सर्ग में प्रकट किया है और नूतन प्रयोगों तथा सिद्धान्तों की चर्चा से यह सिद्ध कर दिया है कि साहित्य के समान ही व्याकरण भी उनका प्रिय विषय था। व्याकरण की नीरस परिभाषाओं का उन्होंने अपनी मनोहर उपमाओं में सुन्दर प्रयोग किया है और मनोहर संयोग बैठाया है। संस्कृत व्याकरण के सूक्ष्म से सूक्ष्म नियमों का भी उन्होंने एकाध स्थलों को छोड़ कर कही भी उल्लंघन नहीं किया है और ऐसे-ऐसे शब्दों को गढ़ कर उनका प्रयोग किया है कि छन्दों की श्रुतिमधुरता बहुत बढ गयी हैं।
कवि के व्याकरण-सम्बन्धी पाण्डित्य के प्रदर्शन के लिए उद्धरणों की कोई आवश्यकता नहीं है। कदाचित् ही ऐसा कोई श्लोक हो जिसमें उसने किसी सुन्दर, सुघड़, किन्तु नूतन (कवियों के प्रयोग मं नूतन) शब्द का प्रयोग न किया हो। व्याकरण-सम्बन्धी प्रसंगों एवं सिद्धान्तों के लिए द्वितीय सर्ग के 47, 112 तथा 19 वे सर्ग के 75 वें श्लोक को देख लेना ही पर्याप्त है।
माघ में पाण्डित्य-प्रदर्शन का शौक अत्यंत दुर्निवार था। कवित्व की सहज शख्ति के साथ ही उनमें पाण्डित्य का स्वाभिमान एवं दूसरों को स्तम्भित करने की इच्छा भी पूर्णतः जागरूक थी। अपने अकेले महाकाव्य को उन्होंने सर्व-साधन-सम्पन्न सम्राट् के एकलौते बेटे की भाँति, अपनी समस्त समृद्धियों एवं शक्तियों से लालित-पालित किया है। अपने पूर्ववर्ती कवियों एवं उनकी कृतियों की समस्त विशेषताओं को आक्रान्त करने की उनमे प्रबल स्पर्धा पाई जाती है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि भारवि की अमर रचना किरातार्जुनीय की बहुत-सी वस्तुओं एवं विशेषताओं को उन्होंने अपने महाकाव्य में भी प्रयुक्त किया है, किन्तु उनसे बीस कर के, उन्नीस कर के नहीं। कहीं पर उसी रूप और प्रकार का अनुसरण कर के उसे रख दिया है तो कहीं पर बिल्कुल नये ढंग और नयी रीति से उसका मुकाबला किया है। दोनों महाकाव्यों में बहुत-सी बातों की समानता पाई जाती है। कुछ समान वस्तुए इस प्रकार है। दोनों ही ने अपने ग्रन्थ के आरम्भ में श्री शब्द से वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोक में यदि भारवि ने लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है तो माघ ने वहाँ भई आरम्भ की तरह श्री शब्द ही प्रयुक्त किया है। भारवि ने किरातार्जुनीय के द्वितीय सर्ग में यदि भीमसेन के संवाद में कुछ राजनीतिक चर्चा की है तो माघ ने उससे कही बढ़ कर बलराम और उद्धव के द्वारा राजनीति की बातें कहलायी है। बारवि ने अपने महाकाव्य की तृतीय सर्ग में अर्जुन के गमन का वर्णन किया है तो माघ ने उसी सर्ग में भगवान् श्रीकृष्ण के गमन का वर्णन किया है। इस प्रसंग पर दोनों ही कवियों ने पुनिवासियों की मार्मिक व्यथाओं का बड़ा मनोहर एवं आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। भारवि ने चतुर्थ और पंचम सर्गों में नगाधिराज हिमालय एवं ऋतुओं का वर्णन अनेक प्रकार के छन्दों में सुन्दर ढंग से किया है तो माघ ने भी उन्हीं सर्गो में रैवतक के प्राकृतिक दृश्यों का मनोहर वर्णन प्रस्तुत किया है। दोनों कवियों ने बड़ी विचित्र समानता के साथ ऋतु वर्णन के प्रसंगों पर तत्तद् वस्तुओं एवं उपादानों को ग्रहण किया है। दोनों ने अपने-अपने महाकाव्यो के आठवे सर्गों में सुन्दरियों की जल-क्रीड़ा का वर्णन तथा नवे और दसवें सर्गो में सायंकाल, चन्द्रोदय, मधुपान, रतिकेलि, प्रणयालाप आदि का श्रृंगारपूर्ण एक-सा वर्णन किया है। एक में यदि वेष्या का प्रसंग है तो दूसरे में भी यादव रमणियाँ है। दोनों कवियों के प्रभात-वर्णन एक ही परम्परा के अनुयायी है। एक में यदि अर्जुन की कठोर तपस्या का हृदयग्राही वर्णन है तो दूसरे में युधिष्ठिर के राजसूर्य यज्ञ का सविधि सविस्तार वर्णन है। दोनों ही महाकाव्यों में युद्धस्थल एवं युद्ध के विविध प्रकारों का रोमांचकारी वर्णन है। युद्धस्थल के प्रसंगों पर दोनों ही कवियों ने विविध प्रकार के विकट चित्रबन्धों द्वारा अपनी प्रचण्ड कवित्व-शक्ति एवं प्रखर प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है। किन्तु इस दिशा में माघ के प्रयोग भारवि की अपेक्षा बहुत सफल हुए है। विविध चित्रबन्धों की विकट कल्पना में एक निपुण वैयाकरण के नाते जो कृतकार्यता माघ को मिली है, वह भारवि को नहीं मिल सकी है।
माघ के कुछ विकट बन्धों के नमूने ये है जिन्हें देखकर पाठकों को दाँतों तले अँगुली दबानी पड़ती है-----
एकाक्षर पाद
जजौजोजाअअजिजिज्जाजी तं ततोअतितताअतितुत्।
भाअअभोअभोभाअभिर्भूभाभूराराअरि ररिरीररः।। सर्ग 19।।3।
इस श्लोक के एक चरण में केवल एक अक्षर का प्रयोग कवि ने किया है, इस प्रकार छन्द के चारों चरणों में केवल चार अक्षरों- ज, त, भ, र- का प्रयोग हुआ है। नीचे के श्लोक केवल दो अक्षरों का प्रयोग हुआ है-----
भूरिभिर्भरिभिभौंरा भूभारैरभिरेभिरे।
भेरीरेभिभिरभ्राअअभैरभीरुभिरिभैरियाः।। सर्ग 19।66।।
अब आगे इससे भी बढ़ कर विस्मयकारी बन्ध देखिए, जिसमें कवि ने केवल एक ही अक्षर का प्रयोग किया है---
बाददो दुद्दबुद्दावी दादो दुददीददोः।
बुद्दादं वददे दुद्दे ददाअददददोअददः।। सर्ग 19।114।।
यह तो हुई अक्षरों की करामात, अब देखिए श्लोक की पहली पूरी पंक्ति ही दूसरी पंक्ति बन गयी है------
सदैव सम्पन्नवपू रणेष महोदधेस्तारि महानितान्सम्।
स दैवसम्पन्नवपूरणेषु महो दधेस्तारिमहा नितान्तम्।। सर्ग 19।118।।
चरणो या पादों के अनुलोम प्रतिलोम के तो बीसों उदाहरण कवि ने प्रस्तुत किये है। सर्वतोभद्र, गोमूत्रिका, अर्धभ्रमक, असंयोग, समुद्गयमक, मुरज-बन्ध, प्रतिलोमानुलोम, गूढ चतुर्थ, तीन अर्थवाची, चार अर्थवाची आदि विकटातिविकट बन्धों की रचना कर कवि ने अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य एवं अद्भुत कवित्व-शक्ति का जो प्रदर्शन किया है, उसका लोहा संस्कृत-समाज में सदा माना जाता रहेगा। यद्यपि इन बन्धों में सर्वत्र कवित्व-रस का मुक्त प्रवाह दूषित हो गया है, और विलप्ट कल्पनाओं एवं बलपूर्वक ग्रहण की जानेवाली अर्थशक्ति का सौन्दर्य घटिया कोटि का हो गया है किन्तु कवि ने जिस दृष्टिकोण से यह कठिन कार्य किया है, उसमे तो वह पर्याप्त सफल माना ही जायेगा।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.
